मूल श्लोक – 9
सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥9॥
शब्दार्थ
- सुहृत् — सच्चा हितैषी, निस्वार्थ भाव से भलाई चाहने वाला
- मित्र — मित्र, सहयोगी
- उदासीन — तटस्थ व्यक्ति, जो न पक्ष में हो न विपक्ष में
- मध्यस्थ — निष्पक्ष न्याय करने वाला, मध्य में रहने वाला
- द्वेष्य — शत्रु, घृणा करने योग्य व्यक्ति
- बन्धुषु — सगे-सम्बंधी, प्रियजन
- साधुषु — सज्जन, धर्मपरायण व्यक्ति
- पापेषु — पापी, अधार्मिक व्यक्ति
- समबुद्धिः — जिसकी बुद्धि सबके प्रति समान है, समदृष्टि रखने वाला
- विशिष्यते — श्रेष्ठ कहा गया है, उत्तम माना जाता है
योगी शुभ चिन्तकों, मित्रों, शत्रुओं पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं।
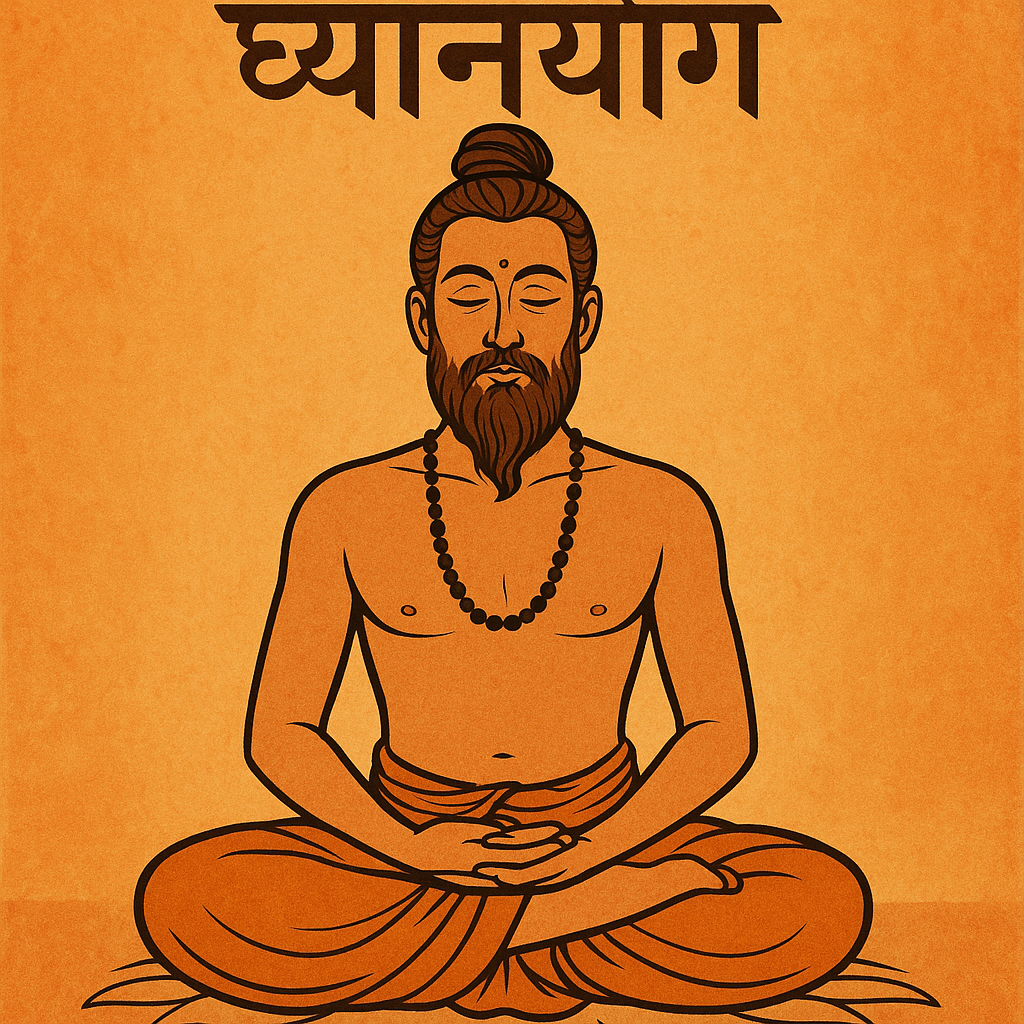
विस्तृत भावार्थ
भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में समदृष्टि या समबुद्धि की महत्ता को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि:
- एक योगी की पहचान यह नहीं कि वह केवल ध्यान करता है, बल्कि यह है कि वह सभी प्रकार के व्यक्तियों के प्रति समान भाव रखता है।
- चाहे वह सच्चा हितैषी हो, मित्र हो, तटस्थ व्यक्ति हो या फिर हमारा विरोधी — योगी उन सभी में एक ही आत्मा के दर्शन करता है।
- उसी प्रकार वह बंधु और शत्रु, धार्मिक और अधार्मिक, सज्जन और पापी – सबके प्रति एक सम दृष्टि रखता है।
- उसका व्यवहार बाहरी गुणों पर आधारित नहीं होता, बल्कि आत्मा की समता पर आधारित होता है।
यह श्लोक इस बात को पुष्ट करता है कि योग का शिखर ‘समत्व’ है, और समत्व का अर्थ है सभी में एक ही परमात्मा को देखना — ‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति’।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- इस श्लोक का सार अद्वैत वेदांत और योगदर्शन दोनों के मूल तत्वों से जुड़ा है।
- अद्वैत कहता है कि सबमें एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, इसलिए भेद की कोई जगह नहीं।
- गीता में यह शिक्षा बार-बार दोहराई जाती है कि राग-द्वेष से मुक्त हो कर ही कोई योगी बन सकता है।
- यह श्लोक हमें मानवीय व्यवहार की उच्चतम चेतना की ओर इंगित करता है — जहाँ हम न प्रशंसा से लिप्त होते हैं, न आलोचना से घृणा करते हैं।
प्रतीकात्मक अर्थ
| शब्द | प्रतीकात्मक अर्थ |
|---|---|
| सुहृत् | निष्कलंक प्रेम करने वाला; जैसे ईश्वर स्वयं |
| मित्र | सामाजिक सहायक, लेकिन कभी-कभी अपेक्षा रखने वाला |
| उदासीन | जो किसी से जुड़ा नहीं, किन्तु विरोधी भी नहीं |
| मध्यस्थ | जीवन के द्वंद्वों में न्याय का प्रतिनिधि |
| द्वेष्य | जो प्रतिकूल है, किन्तु फिर भी आत्मस्वरूप में सम है |
| बन्धु | पारिवारिक मोह से जुड़ा व्यक्ति |
| साधु | धर्मनिष्ठ, नैतिक, उच्च आचरण वाला व्यक्ति |
| पापी | नैतिक पतन से युक्त, किन्तु फिर भी आत्मा से युक्त व्यक्ति |
| समबुद्धि | समता की दृष्टि जिसमें सभी एक ही आत्मा के रूप में देखे जाते हैं |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- सच्चा योग केवल ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि यह है कि हम सभी के साथ एक समान दृष्टि रखें।
- व्यक्तियों के कर्म भिन्न हो सकते हैं, पर आत्मा एक ही है — यही दृष्टि योगी की होती है।
- यदि हम किसी को पापी या शत्रु कहकर घृणा करते हैं, तो हम आत्मज्ञान से दूर हैं।
- समदृष्टि ही सच्चे भक्ति और ज्ञान का प्रतिफल है।
- यह समता नैतिक श्रेष्ठता नहीं, बल्कि अद्वैत चेतना का अनुभव है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
- क्या मैं दूसरों को केवल उनके कर्मों से आंकता हूँ या उनकी आत्मा को भी देखता हूँ?
- क्या मैं अपने शत्रु या विरोधी को भी आत्मा के दृष्टिकोण से देख पाता हूँ?
- क्या मेरे व्यवहार में पक्षपात या द्वेष होता है?
- क्या मैं सज्जनों और पापियों दोनों के प्रति समभाव रख पाता हूँ?
- क्या मेरा योग केवल ध्यान तक सीमित है या वह व्यवहार में भी समता को प्रकट करता है?
निष्कर्ष
यह श्लोक गीता के समत्व योग की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है।
श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि योग का सर्वोच्च लक्षण है — समबुद्धि।
जो व्यक्ति सभी के प्रति एक जैसा भाव रखे — चाहे वे हितैषी हों या विरोधी, सज्जन हों या पापी — वही वास्तव में सिद्ध योगी है।
योग का सार यही है:
“सभी में ईश्वर को देखो, भले ही वे तुम्हारे शत्रु हों या सखा — क्योंकि आत्मा एक है, परमात्मा एक है।”
यह दृष्टिकोण ही आत्मज्ञान है, मोक्ष का आधार है, और जीवन की पूर्णता है।
