मूल श्लोक: 60
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥
शब्दार्थ
- यततः — प्रयास करते हुए
- हि — निःसंदेह
- अपि — भी
- कौन्तेय — हे कुन्तीपुत्र (अर्जुन)
- पुरुषस्य — मनुष्य का
- विपश्चितः — ज्ञानी, विवेकी
- इन्द्रियाणि — इन्द्रियाँ
- प्रमाथीनि — अत्यंत चंचल, बलवान
- हरन्ति — हर लेती हैं, खींच लेती हैं
- प्रसभम् — बलपूर्वक
- मनः — मन को
हे कुन्ती पुत्र! इन्द्रियाँ इतनी प्रबल और अशान्त होती हैं कि वे विवेकशील और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी वरवश में कर लेती है।
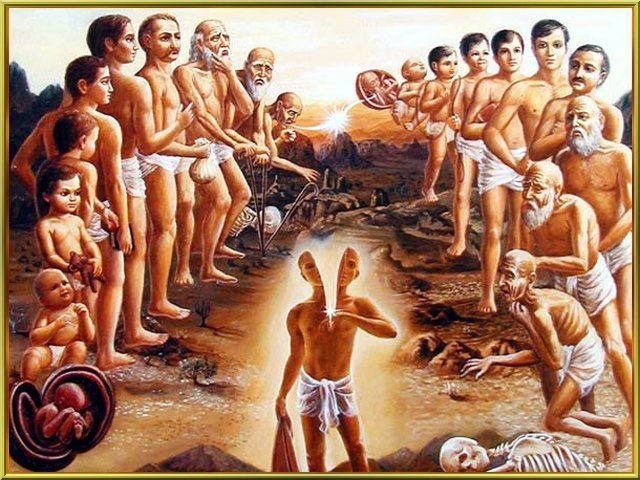
विस्तृत भावार्थ
श्रीकृष्ण यहाँ एक गंभीर आध्यात्मिक सतर्कता की ओर संकेत कर रहे हैं:
- केवल ज्ञान और विवेक होना पर्याप्त नहीं है,
- जब तक इन्द्रियाँ संयमित नहीं होतीं,
- तब तक वे मन को खींचकर विषयों में उलझा देती हैं, चाहे साधक कितना भी प्रयासरत क्यों न हो।
यह श्लोक मानव मन की अस्थिरता और इन्द्रियों की शक्ति को स्पष्ट करता है।
भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण
‘यततः हि अपि’ — प्रयासरत होने पर भी
- साधक चाहे निरंतर अभ्यास करे,
- आत्म-नियंत्रण में लगे रहे,
- परन्तु पूर्ण सावधानी और निरंतर सजगता के बिना इन्द्रियाँ उसका ध्यान भटका सकती हैं।
यहाँ श्रीकृष्ण यह नहीं कह रहे कि प्रयास व्यर्थ है,
बल्कि यह बता रहे हैं कि:
आत्म-संयम एक सतत युद्ध है, जिसमें किसी क्षण भी ढिलाई नहीं हो सकती।
‘विपश्चितः’ — विवेकी पुरुष
- ज्ञानवान व्यक्ति भी यदि इन्द्रियों के प्रभाव को हल्के में ले,
- तो वह भी माया के जाल में फँस सकता है।
विवेक का अर्थ केवल शास्त्र ज्ञान नहीं,
बल्कि इन्द्रियों पर निरंतर जागरूक नियंत्रण भी है।
‘प्रमाथीनि’ — अत्यंत चंचल और बलशाली इन्द्रियाँ
- इन्द्रियाँ (नेत्र, कान, जिव्हा आदि)
- अत्यंत चंचल, बलवान, और मन को भ्रमित करने में कुशल हैं।
इनका स्वभाव ही है:
- विषयों की ओर भागना,
- आकर्षण में उलझना,
- और साधक के मन को विचलित करना।
‘हरन्ति प्रसभं मनः’ — बलपूर्वक मन को खींच लेना
- यह चेतावनी है:
- यदि सजगता में कमी आई,
- तो इन्द्रियाँ मन को खींचकर विषयों में उलझा देंगी।
साधक फिर से आसक्ति, मोह, क्रोध, और भटकाव में फँस सकता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- ज्ञान और साधना के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती इन्द्रिय-नियंत्रण है।
- केवल शास्त्र पढ़ लेना या बुद्धि से समझ लेना पर्याप्त नहीं।
- जागरूकता, सतत अभ्यास, और वैराग्य आवश्यक हैं।
गीता यहाँ एक वास्तविकता को स्वीकार करती है —
कि इन्द्रियाँ बलवान हैं, और उनसे मुकाबला आसान नहीं।
इसलिए आत्मसाधना में विनम्रता, सावधानी, और निरंतरता चाहिए।
प्रतीकात्मक अर्थ
- यततः पुरुषः — साधक, योगी
- विपश्चितः — ज्ञानयुक्त
- इन्द्रियाणि — विषय-आकर्षण के माध्यम
- प्रमाथीनि — विनाशकारी यदि संयम न हो
- हरन्ति मनः — चेतना को विषयों की ओर खींच ले जाती हैं
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- आध्यात्मिक साधना में इन्द्रिय-संयम अत्यंत आवश्यक है।
- ज्ञान, तप, ध्यान — सब व्यर्थ हो सकते हैं यदि इन्द्रियाँ असंयमित रहें।
- यह श्लोक साधकों को निरंतर सजग रहने की चेतावनी देता है।
इन्द्रियाँ:
- छोटे-छोटे रूपों में आकर्षण दिखाती हैं,
- और मन को विषयों में खो देने के लिए मजबूर करती हैं।
इसलिए योग और संयम का अभ्यास सतत रूप से आवश्यक है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मैं अपनी इन्द्रियों को पूर्णतः संयमित रख पा रहा हूँ?
क्या मुझे कभी ऐसा लगा कि विषयों ने मुझे विवेक होते हुए भी अपनी ओर खींच लिया?
क्या मैं साधना में नियमित और सजग हूँ?
क्या मेरा मन इन्द्रिय विषयों में उलझकर मेरी आत्मिक उन्नति को रोकता है?
क्या मैं केवल ज्ञान से संतुष्ट हूँ, या उसे अभ्यास में लाने का प्रयास भी करता हूँ?
निष्कर्ष
यह श्लोक हमें मानव जीवन के सबसे बड़े संघर्ष — इन्द्रिय संयम की ओर सावधान करता है।
- यह बताता है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल विचार या शास्त्रज्ञान से नहीं होती,
- बल्कि मन और इन्द्रियों के ऊपर सजग नियंत्रण से होती है।
योगी वही है जो:
- इन्द्रियों की गति को पहचानता है,
- सजग रहकर उन्हें नियंत्रित करता है,
- और बार-बार मन को आत्मा की ओर खींचता है।
“ज्ञान प्राप्त करना कठिन है,
लेकिन उससे भी कठिन है — उस ज्ञान को इन्द्रियों के माध्यम से नष्ट न होने देना।”
जो इस मार्ग पर अडिग रहता है, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है — और वही मोक्ष का अधिकारी बनता है।
