मूल श्लोक: 64
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥
शब्दार्थ
- रागद्वेषवियुक्तैः — प्रेम (राग) और द्वेष (घृणा) से रहित
- तु — किन्तु, परन्तु
- विषयान् — विषयों को (इन्द्रिय विषयों को)
- इन्द्रियैः — इन्द्रियों के द्वारा
- चरन् — विचरित, सक्रिय
- आत्मवश्यैः — अपनी आत्मा के नियंत्रण में, आत्मसंयमी
- विधेयात्मा — आज्ञाकारी, नियम का पालन करने वाला मन
- प्रसादम् — शान्ति, स्थिरता, प्रसन्नता
- अधिगच्छति — प्राप्त करता है, संपादित करता है
लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इन्द्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है।
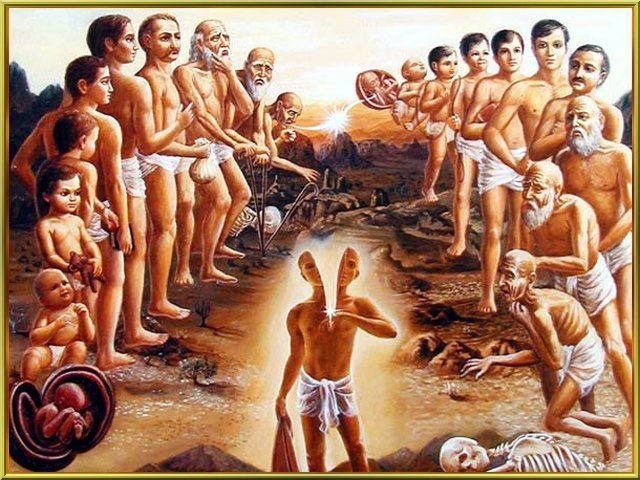
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में श्रीकृष्ण बताते हैं कि मनुष्य जब इन्द्रिय विषयों के संपर्क में रहता है, परन्तु उसे राग (आसक्ति) और द्वेष (नफ़रत) से मुक्त रखता है, तब वह अपने मन को नियंत्रित करके मानसिक शांति और प्रसन्नता की अवस्था प्राप्त कर सकता है।
राग और द्वेष, ये दो विपरीत भाव हैं, जो मन के अस्थिरता और विक्षोभ का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों से रहित होकर विषयों का अनुभव करता है, तो उसका मन संकुचित नहीं होता, वह स्वतः संतुलित रहता है।
“आत्मवश्यैः विधेयात्मा” शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति अपने मन और इन्द्रियों का अधीन है, अर्थात मन और इन्द्रिय उसके वश में हैं, न कि वह मन और इन्द्रिय के अधीन है। ऐसा मन नियंत्रण, आज्ञाकारिता और संयम की भावना रखता है।
“प्रसादमधिगच्छति” का अर्थ है – ऐसी स्थिति प्राप्त करता है जहाँ मन प्रसन्न, शान्त और स्थिर रहता है। इसे शास्त्रों में “समाधि” या “सिद्धि” की अवस्था भी कहा गया है।
भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण
दार्शनिक दृष्टिकोण
यह श्लोक मन की उच्च स्थिति का परिचायक है, जहाँ मनुष्य ने राग-द्वेष के बंधन तोड़ लिए हैं। विषयों से न तो वह आकर्षित होता है, न ही उनसे द्वेष रखता है। वह निष्पक्ष भाव से जीवन की परिस्थितियों का अनुभव करता है।
यह शांति की अवस्था ‘प्रसाद’ है, जो मन के अंदर की गहरी स्थिरता और संतोष को दर्शाती है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी संसार की उथल-पुथल से अप्रभावित रहता है और आत्मा के स्वभाव के अनुसार चलता है।
प्रतीकात्मक अर्थ
- रागद्वेषवियुक्तः — संतुलित मन, जो प्रेम और द्वेष के बिना विषयों का अनुभव करता है।
- विषयानिन्द्रियैः — इन्द्रिय विषयों का संयमित उपयोग।
- आत्मवश्यम् — आत्म-नियंत्रण, मन और इन्द्रियों का नियंत्रण।
- प्रसादः — मानसिक स्पष्टता, शांति और आनन्द।
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- इन्द्रिय विषयों से पूर्ण विरक्ति संभव न हो तो कम से कम राग-द्वेष रहित दृष्टि अपनानी चाहिए।
- आत्मसंयम और मन की आज्ञाकारिता से मानसिक शांति प्राप्त होती है।
- मन की प्रसन्नता और स्थिरता आत्मज्ञान का लक्षण है।
- जीवन के सुख-दुख में समत्व और संतुलन बनाए रखना श्रेष्ठ आध्यात्मिक लक्ष्य है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मैं विषयों का अनुभव करते हुए भी अपने मन में प्रेम और द्वेष से मुक्त हूँ?
क्या मैं अपने इन्द्रिय और मन को नियंत्रित कर पाता हूँ?
क्या मैं जीवन की परिस्थितियों में स्थिर और प्रसन्न रह पाता हूँ?
क्या मेरा मन आज्ञाकारी और संयमी है या क्षणिक भावनाओं का शिकार होता है?
क्या मैं मानसिक प्रसाद की उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ?
निष्कर्ष
यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन की शांति और प्रसन्नता का मूल राग-द्वेष से मुक्त होना है। जब हम विषयों में लीन होते हुए भी अपने मन को नियंत्रण में रख लेते हैं, तब हम स्थिरता और आनंद की अवस्था में पहुँचते हैं।
गीता की यह शिक्षा हमें इन्द्रिय विषयों के मोह-माया से बाहर निकलकर एक संतुलित, संयमी और शान्तचित्त जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। ऐसे मनुष्य का जीवन न केवल आत्मिक होता है बल्कि वह संसार में भी स्थिर और प्रसन्नचित्त रहता है।
इस प्रकार, राग-द्वेषविहीन भाव से विषयों का अनुभव करना और आत्मा को वश में रखना परम योग का स्वरूप है।
