मूल श्लोक: 27
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥27॥
शब्दार्थ
- सर्वाणि — सभी
- इन्द्रिय-कर्माणि — इन्द्रियों के कार्य (जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि)
- प्राण-कर्माणि — प्राण से संबंधित कार्य (जैसे श्वास लेना, छोड़ना, पाचन, उत्सर्जन आदि)
- च — और
- अपरे — कुछ अन्य योगीजन
- आत्म-संयम-योग-अग्नौ — आत्म-संयम रूपी योग की अग्नि में
- जुह्वति — आहुति देते हैं, अर्पण करते हैं
- ज्ञान-दीपिते — ज्ञान से प्रकाशित (प्रज्ज्वलित)
दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इन्द्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं।
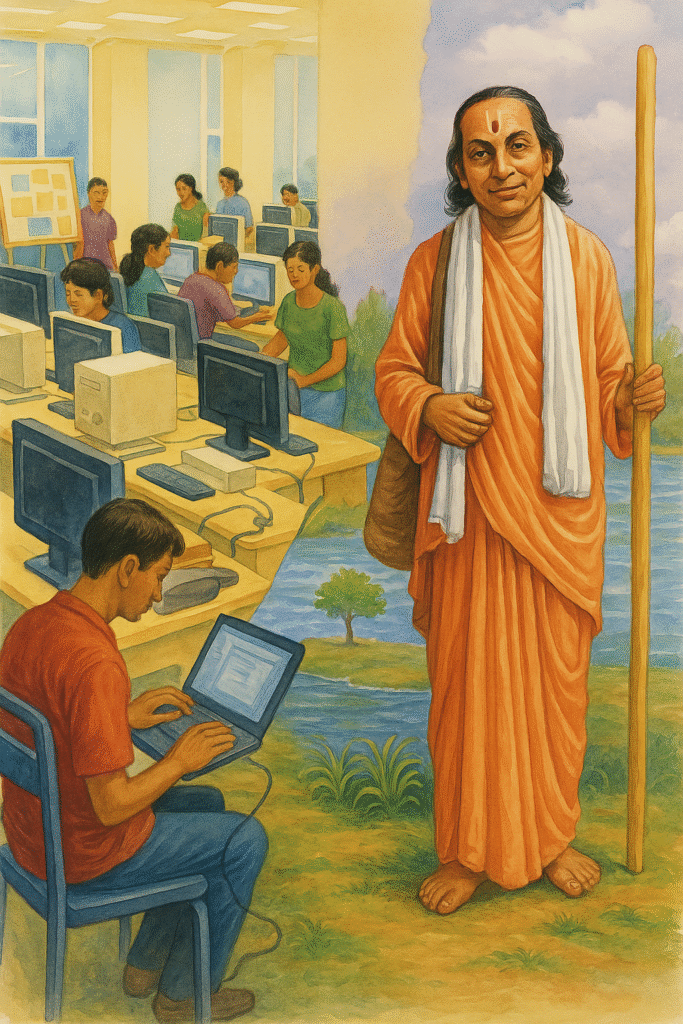
विस्तृत भावार्थ
भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में उस उच्च कोटि के योगीजन की चर्चा कर रहे हैं जो अपने समस्त इन्द्रिय-कर्म (जैसे देखना, बोलना, सुनना, आदि) और प्राण-कर्म (जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संचरण आदि) को आत्मसंयम और योग साधना की अग्नि में आहुति देकर, उन्हें ज्ञान में रूपांतरित करते हैं।
यह श्लोक बाह्य और आंतरिक यज्ञों से आगे बढ़कर “आत्मिक यज्ञ” की बात करता है — जहाँ साधक अपने समस्त क्रियाओं को त्याग और संयम के माध्यम से ईश्वरार्पण करता है।
भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण
योग की उच्च अवस्था
यह श्लोक एक ऐसे साधक का चित्रण करता है जो न केवल बाह्य कर्मों का नियंत्रण करता है, बल्कि अपनी समस्त जीवन-शक्ति (प्राणशक्ति) और ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी संयम के द्वारा आत्मवश करता है।
उसके लिए देखना, सुनना, बोलना भी एक प्रकार का यज्ञ है — वह इन क्रियाओं को भोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि ईश्वरार्पण और आत्मविकास की दृष्टि से करता है।
ज्ञानदीपित अग्नि
साधक की आत्मा में जब ज्ञान का दीपक जल उठता है, तब उसकी समस्त क्रियाएं उस ज्ञान से प्रकाशित हो जाती हैं। यह अग्नि कामनाओं से नहीं, बल्कि आत्मबोध, विवेक और त्याग से प्रज्वलित होती है।
ज्ञानदीपित अग्नि का तात्पर्य है वह अंतर्मन की चेतना जो अज्ञान के अंधकार को जला देती है।
संयम और आत्मार्पण
संयम ही वह अग्नि है जिसमें इन्द्रिय और प्राण की समस्त क्रियाएं आहुत होती हैं। साधक अब भोग के लिए नहीं, मोक्ष और ब्रह्मज्ञान के लिए कर्म करता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
यज्ञ का आंतरिक स्वरूप
यह श्लोक स्पष्ट करता है कि यज्ञ केवल अग्निहोत्र तक सीमित नहीं है। जब साधक अपनी इन्द्रियों और प्राणों की प्रवृत्तियों को ज्ञानपूर्वक संयमित करता है, और उन्हें आत्मनियंत्रण में लाता है — तभी वास्तविक यज्ञ होता है।
कर्म का दिव्य रूपांतरण
जब कर्म संयम और ज्ञान से जुड़ जाए, तो वह साधारण न रहकर दिव्य बन जाता है। उस अवस्था में सभी क्रियाएँ मोक्ष का साधन बन जाती हैं, बन्धन का नहीं।
योग की परिपक्व अवस्था
यह श्लोक योग की उस अवस्था का वर्णन करता है जहाँ साधक स्वयं को समर्पित कर देता है — कर्म, इन्द्रियाँ, प्राण, विचार, सब कुछ — ब्रह्म के पथ में।
प्रतीकात्मक अर्थ
| प्रतीक | अर्थ |
|---|---|
| इन्द्रियकर्म | देखने, सुनने, बोलने, आदि की क्रियाएँ |
| प्राणकर्म | श्वसन, पाचन, रक्तसंचार, आदि की क्रियाएँ |
| आत्मसंयम | संयम, नियंत्रण, निग्रह |
| योगाग्नि | योग की अग्नि — समर्पण और त्याग |
| ज्ञानदीपित | आत्मबोध से प्रकाशित — विवेक से जलती हुई चेतना |
| जुह्वति | आहुति देना — आत्मार्पण करना |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- आत्मसंयम ही सर्वोच्च यज्ञ है।
- केवल बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं — प्राण और मन के स्तर पर भी संयम आवश्यक है।
- ज्ञान के प्रकाश में ही संयम और त्याग फलदायक होते हैं।
- प्रत्येक कर्म को यज्ञ की भावना से करना चाहिए।
- संयम और विवेकपूर्ण आचरण ही मोक्ष का मार्ग है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मेरी इन्द्रियाँ मेरे वश में हैं या मैं उनके वश में हूँ?
क्या मैं अपने प्राण और मन पर नियंत्रण रखता हूँ?
क्या मैं अपनी हर क्रिया को यज्ञ रूप में देखता हूँ?
क्या मेरी साधना केवल बाह्य है, या आंतरिक भी?
क्या मैंने अपने भीतर ज्ञानदीप जलाया है?
निष्कर्ष
यह श्लोक श्रीकृष्ण के द्वारा यज्ञ के गूढ़तम स्वरूप को स्पष्ट करता है। बाह्य हवन की तुलना में आत्मसंयम रूपी यज्ञ कहीं अधिक श्रेष्ठ और स्थायी है।
जब साधक अपनी इन्द्रियों की हर क्रिया और प्राण की हर गति को ब्रह्म के प्रति समर्पित करता है, तभी वह सच्चे अर्थ में योगी बनता है।
यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है — जिसमें साधक निरंतर ईश्वर के लिए जीता है, कर्म करता है और प्रत्येक क्षण को यज्ञ में परिवर्तित करता है।
इस प्रकार, “ज्ञानदीपित आत्मसंयम की अग्नि” में जब इन्द्रियों और प्राणों की आहुति दी जाती है, तो मनुष्य समस्त बन्धनों से मुक्त होकर ईश्वर के समीप पहुँचता है — यही मोक्ष है।
