मूल श्लोक: 30
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः॥
शब्दार्थ
- अपरे — अन्य साधक
- नियत-आहाराः — नियमित व नियंत्रित आहार लेने वाले
- प्राणान् — प्राणों को (वायु या जीवनशक्ति को)
- प्राणेषु — अन्य प्राणों में (वायु प्रवाहों में)
- जुह्वति — आहुति देते हैं, अर्पण करते हैं
- सर्वे अपि एते — ये सभी
- यज्ञविदः — यज्ञ की वास्तविक विधियों को जानने वाले
- यज्ञ-क्षपित-कल्मषाः — यज्ञों द्वारा पापों से मुक्त हुए
कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणामस्वरूप साधक स्वयं को शुद्ध करते हैं।
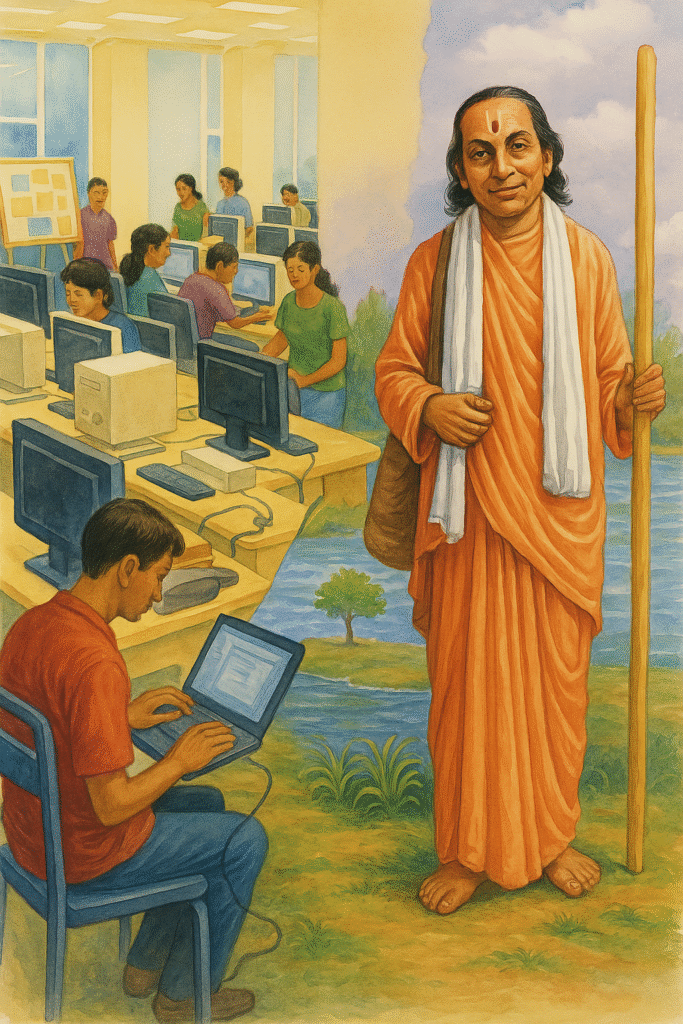
विस्तृत भावार्थ
भगवान श्रीकृष्ण यहाँ यज्ञ के और एक विशेष प्रकार की साधना का उल्लेख करते हैं — प्राणायाम रूप यज्ञ, जिसमें साधक अपनी प्राणवायु (श्वास) को नियंत्रित कर प्राण और अपान वायु में आहुति देता है।
नियत आहार का महत्व
“नियताहार” शब्द बहुत गहरा है। इसका अर्थ केवल नियमित समय पर भोजन करना नहीं है, बल्कि —
- सात्त्विक भोजन करना
- संयमित मात्रा में करना
- इन्द्रिय-भोग के लिए नहीं, जीवन निर्वाह के लिए खाना
- ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से भोजन करना
जब व्यक्ति अपने आहार को संयमित करता है, तब उसका मन और शरीर दोनों साधना के योग्य बनते हैं। यही कारण है कि योगशास्त्र में आहार को साधना का मूल आधार माना गया है।
प्राणायाम यज्ञ की प्रक्रिया
यह वह साधना है जिसमें व्यक्ति श्वासों को नियंत्रित करके, यानी पूरक, कुम्भक, रेचक के माध्यम से अपनी जीवनशक्ति (प्राण) को भीतर ही संयमित करता है।
- प्राण — जो बाहर से अंदर की ओर गति करता है (श्वास लेना)
- अपान — जो भीतर से बाहर की ओर गति करता है (श्वास छोड़ना)
इन दोनों को एक-दूसरे में आहुति देने का अर्थ है — श्वासों को इस प्रकार नियंत्रित करना कि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाएँ।
यज्ञ के फलस्वरूप क्या होता है?
श्रीकृष्ण कहते हैं कि इन सभी साधकों ने यज्ञ के ज्ञान को प्राप्त किया है और अपने पापों को यज्ञ के माध्यम से जला दिया है।
इसका भाव यह है कि जब साधना शुद्ध होती है, और उसमें त्याग, श्रद्धा, संयम तथा नियमितता होती है, तो वह साधक को आत्मिक शुद्धि प्रदान करती है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश यह है कि —
- सच्चा यज्ञ वह है, जिसमें हम अपने अहंकार, वासनाओं, आसक्तियों, सांसारिक लालसाओं को अर्पण करें।
- शारीरिक यज्ञ (हवन, अग्निहोत्र) जितना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्राण यज्ञ, मन यज्ञ और आत्म यज्ञ भी है।
- प्राणायाम के माध्यम से जब साधक अपने श्वासों पर नियंत्रण करता है, तो वह न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि अपने मन को एकाग्र भी करता है — जो ब्रह्मज्ञान के लिए अनिवार्य है।
नियत आहार भी केवल भोजन का विषय नहीं है, बल्कि यह संयम की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने आहार पर नियंत्रण रख सकता है, वह धीरे-धीरे अपनी इन्द्रियों, मन और अंततः अपने कर्मों पर भी नियंत्रण पा लेता है।
प्रतीकात्मक अर्थ
- प्राण — जीवनशक्ति, चेतना
- जुह्वति — समर्पण करना, अर्पित करना
- नियताहार — शरीर व मन दोनों में संयम
- यज्ञविदः — जो साधना के गूढ़ तत्व को समझते हैं
- कल्मष — पाप, अशुद्धियाँ
- यज्ञ-क्षपित — यज्ञ रूपी अग्नि से नष्ट किया हुआ
इस प्रकार, यह श्लोक बाहरी कर्मकांड से हटकर आंतरिक साधना की महत्ता को रेखांकित करता है।
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- भोजन पर नियंत्रण साधना की पहली सीढ़ी है।
- प्राणायाम मात्र श्वास का खेल नहीं, यह चेतना का गहरा अभ्यास है।
- शुद्ध साधना के द्वारा ही व्यक्ति अपने भीतर के दोषों को दूर कर सकता है।
- सभी यज्ञों का मूल है त्याग और संयम।
- बाहरी अग्नि में आहुति देने से अधिक महत्वपूर्ण है — अहंकार को अंतःकरण की अग्नि में जलाना।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मेरा भोजन संयमित और सात्त्विक है?
क्या मैं अपनी प्राणशक्ति को नियंत्रित कर पा रहा हूँ या वह व्यर्थ नष्ट हो रही है?
क्या मैं केवल बाहरी यज्ञ करता हूँ या मन और प्राण को भी समर्पित करता हूँ?
क्या मेरी साधना मेरे दोषों को जलाने में समर्थ हो रही है?
क्या मैं यज्ञ का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ या केवल उसकी विधि तक सीमित हूँ?
निष्कर्ष
भगवद्गीता का यह श्लोक हमें साधना की आंतरिक गहराइयों से परिचित कराता है। श्रीकृष्ण यह बताना चाहते हैं कि यज्ञ केवल अग्निकुंड में हवन करना नहीं है, बल्कि अपने प्राणों का संयम, अपने आहार का शुद्धिकरण, और अपने मन का समर्पण भी यज्ञ का ही रूप है।
जो व्यक्ति इस प्रकार की साधना में लीन होता है, वह न केवल शरीर और मन की शुद्धि करता है, बल्कि अपने पापों को यज्ञाग्नि में जला देता है।
यह श्लोक साधकों के लिए एक प्रेरणा है — बाह्य क्रियाओं से भीतर की साधना तक पहुँचने की।
