मूल श्लोक– 7
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥
शब्दार्थ (शब्दों का संक्षिप्त अर्थ)
- योगयुक्तः — योग से युक्त, परमात्मा में स्थिर
- विशुद्धात्मा — शुद्ध अंतःकरण वाला, निर्मल आत्मा
- विजितात्मा — जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है
- जितेन्द्रियः — जिसकी इन्द्रियाँ वश में हैं
- सर्वभूतात्मभूतात्मा — जो सब प्राणियों में आत्मा रूप में स्थित आत्मा को पहचानता है
- कुर्वन् अपि — कर्म करते हुए भी
- न लिप्यते — लिप्त नहीं होता, बाँधता नहीं है
जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इन्द्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्मबंधन में नहीं पड़ते।
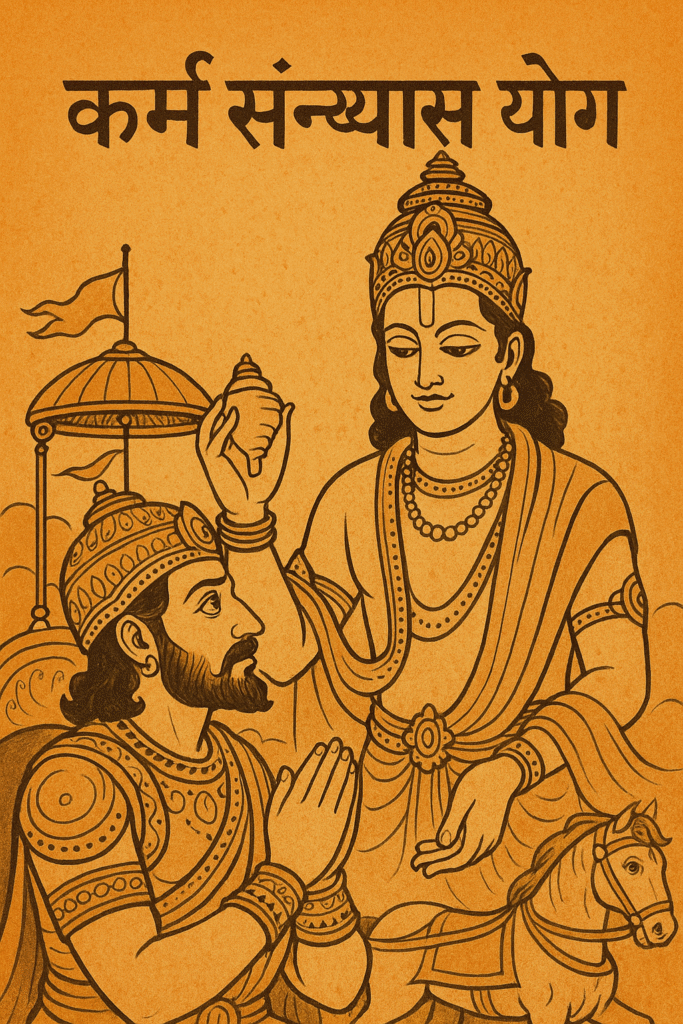
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण योगी की एक आदर्श अवस्था का वर्णन करते हैं। जो साधक योग में स्थिर है, उसकी आत्मा विशुद्ध है। उसने अपने मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखता है — ‘एकत्व’ की दृष्टि से युक्त होता है।
ऐसा साधक कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्म को कर्तापन और फलों की आसक्ति से मुक्त होकर करता है। उसका कार्य बंधनकारक नहीं होता।
इस अवस्था का साधक संसार में रहता है, कार्य करता है, लेकिन भीतर से वह निर्लिप्त रहता है, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- योगयुक्तता का अर्थ केवल आसनों या ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो ब्रह्म से जुड़ी है।
- विशुद्धात्मा होने का अर्थ है — अहंकार, राग, द्वेष आदि विकारों से मुक्त होना।
- विजितात्मा और जितेन्द्रिय दर्शाते हैं कि आत्म-संयम ही आत्मज्ञान का आधार है।
- सर्वभूतात्मभूतात्मा — अद्वैत दर्शन का उच्चतम सूत्र: सब में उसी आत्मा को देखना जो अपने भीतर है।
- कर्म करते हुए ‘न लिप्यते’ — यह निष्काम कर्मयोग की चरम अवस्था है, जहाँ साधक कार्य करता है, लेकिन उसमें अहंकार और ममता नहीं होती।
प्रतीकात्मक अर्थ
- योगयुक्तः — वह जिसकी चेतना आत्मा में स्थिर है, जो अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ चुका है।
- विशुद्धात्मा — ऐसा अंतःकरण जो आत्मसाक्षात्कार से पारदर्शी हो चुका है।
- विजितात्मा — अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण पा चुका साधक।
- जितेन्द्रियः — इन्द्रिय-विजयी व्यक्ति, जो विषयों के आकर्षण से प्रभावित नहीं होता।
- सर्वभूतात्मभूतात्मा — जो इस ब्रह्मांड में सभी प्राणियों को एक ही चेतन सत्ता का अंश मानता है।
- न लिप्यते — ऐसा व्यक्ति बाह्य कर्मों के फल या बंधन में नहीं फँसता।
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- योग का अर्थ केवल साधना नहीं, जीवन की दृष्टि है — जहाँ हर कर्म को ब्रह्मार्पण किया जाता है।
- भीतर की शुद्धता बाहरी कर्मों को दिव्य बना देती है — विशुद्धात्मा का कर्म बंधन नहीं रचता।
- संयम आत्मा को मुक्त करता है — इन्द्रियों और मन पर नियंत्रण आत्म-साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है।
- समदृष्टि ही दिव्यता का परिचायक है — सभी में एक ही आत्मा को देखना, अहिंसा और प्रेम का मूल है।
- कर्म का बंधन मन की लिप्सा से है — कर्म नहीं बाँधता, भावनाएं और आसक्ति बाँधती हैं।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मैं अपने मन और इन्द्रियों को नियंत्रित कर पाया हूँ?
क्या मेरे कर्म किसी अपेक्षा या मान्यता से प्रेरित हैं?
क्या मैं सभी में एक ही आत्मा को देख पाता हूँ?
क्या मैं कर्म करते हुए भी भीतर से शांत और निर्लिप्त रह पाता हूँ?
क्या मेरा योग केवल अभ्यास तक सीमित है या जीवन की दृष्टि बन चुका है?
निष्कर्ष
यह श्लोक गीता के कर्मयोग दर्शन का सार है। योगयुक्त, संयमी, और शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसमें नहीं फँसता। वह संसार में रहते हुए, सभी से प्रेम करते हुए, सभी में आत्मा को देखते हुए — मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है।
ऐसा व्यक्ति ‘जीवन-मुक्त’ होता है — वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसमें नहीं रहता। यही गीता का दिव्य संदेश है — कर्म करते हुए भी आत्मा में स्थित हो जाना।
“जो समदृष्टि, संयम और योग से युक्त है — वही संसार में रहते हुए भी मुक्त है।”
