मूल श्लोक – 7
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥7॥
शब्दार्थ
- जितात्मनः — जिसने अपने मन और इन्द्रियों को वश में कर लिया है
- प्रशान्तस्य — जिसका चित्त शांत है
- परमात्मा — परम सत्ता, परमेश्वर
- समाहितः — केंद्रित, समाहित, स्थित
- शीत — सर्दी
- उष्ण — गर्मी
- सुख-दुःखेषु — सुख और दुःख में
- तथा — और
- मान-अपमानयोः — सम्मान और अपमान में
वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है वे शीत-ताप, सुख-दुख और मान-अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शान्त रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है।
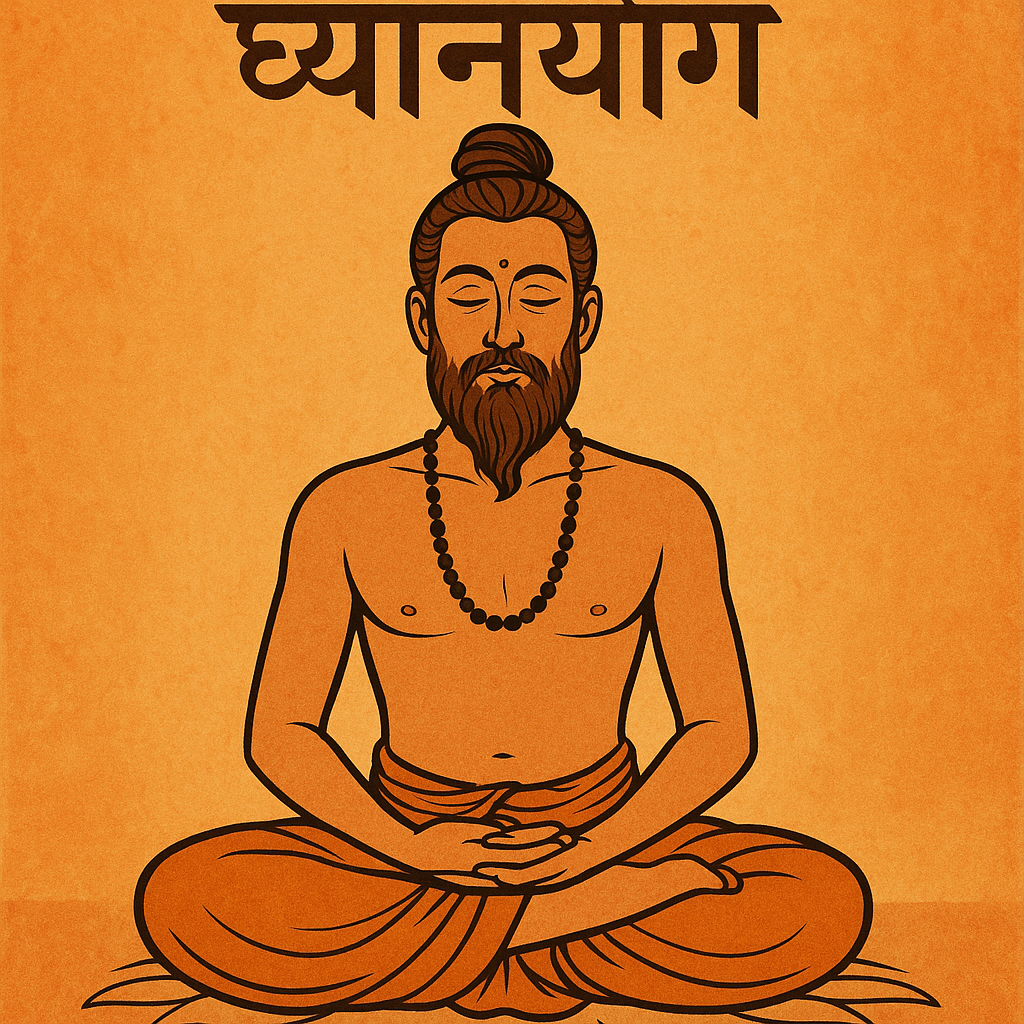
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण उस योगी की स्थिति का वर्णन करते हैं जो आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। श्रीकृष्ण के अनुसार:
- जो साधक जितात्मा है — अर्थात जिसने अपने मन और इन्द्रियों को वश में कर लिया है,
- जो प्रशांत है — यानी जिसका चित्त राग-द्वेष, क्रोध, मोह आदि से मुक्त होकर पूरी तरह शांत हो गया है,
- उसी के लिए परमात्मा आत्मा में समाहित हो जाते हैं — अर्थात ऐसा व्यक्ति परमात्मा के साक्षात अनुभव में स्थित हो जाता है।
इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि परमात्मा का साक्षात्कार केवल वही कर सकता है जिसकी भीतर की अवस्था स्थिर और शांत हो, जो जीवन के सुख-दुख, मान-अपमान, गर्मी-ठंडी जैसी द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- मन की स्थिरता ही ईश्वर-प्राप्ति का आधार है।
- श्रीकृष्ण यह बता रहे हैं कि जब तक हम अपने अंतर्मन के द्वंद्वों पर विजय नहीं पाते, तब तक परमात्मा हमारे भीतर स्थित नहीं हो सकते।
- परमात्मा बाहर नहीं, भीतर स्थित हैं, लेकिन उन्हें अनुभव करने के लिए मन को जितना और शांत करना अनिवार्य है।
- शीत-उष्ण, सुख-दुख, मान-अपमान — ये सभी द्वंद्वात्मक अनुभव हैं जो मनुष्य को विचलित करते हैं, और जब तक इनका असर हमारे भीतर होता है, तब तक आत्मा परमात्मा से विलग रहती है।
- समता — गीता का मूल दर्शन — इस श्लोक में अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है।
प्रतीकात्मक अर्थ
| शब्द | प्रतीकात्मक अर्थ |
|---|---|
| जितात्मा | जिसने अपनी इच्छाओं, वासनाओं, इन्द्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो |
| प्रशांत | राग-द्वेष से मुक्त, अंतर्मन में पूर्ण शांत |
| परमात्मा समाहितः | परम सत्ता का आत्मा में साक्षात निवास, ब्रह्म की चेतना में स्थिर होना |
| शीत-उष्ण | जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलता, भौतिक परिवर्तन |
| सुख-दुःख | संवेदनात्मक अनुभव जो मनुष्य की चेतना को हिलाते हैं |
| मान-अपमान | अहंकार और सामाजिक पहचान से जुड़े अनुभव, जिनसे मन को विक्षोभ होता है |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- आत्मविजय ही ईश्वरदर्शन की कुंजी है।
जब तक मनुष्य अपनी वासनाओं और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करता, तब तक परमात्मा का अनुभव दूर रहता है। - शांति बाहरी नहीं, आंतरिक दशा है।
यह चित्त की अवस्था है, जो केवल साधना, संयम और विवेक से प्राप्त होती है। - ईश्वरप्राप्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन की चरम अवस्था है।
जब व्यक्ति सभी द्वंद्वों में समान भाव रखता है, तब उसका मन परमात्मा के लिए उपयुक्त पात्र बनता है। - सुख-दुख और मान-अपमान जैसी स्थितियाँ स्थायी नहीं हैं, इनका आना-जाना तय है।
इनसे समभाव रखना ही आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। - परमात्मा को पाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अंतर्मन को देखने और साधने की जरूरत है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
- क्या मैंने अपने मन और इन्द्रियों को नियंत्रित किया है या वे मुझे नियंत्रित करते हैं?
- क्या मेरे भीतर शांति है, या मैं बाहरी घटनाओं से प्रभावित होता रहता हूँ?
- क्या मैं सुख और दुख, मान और अपमान, गर्मी और सर्दी — इन सभी अनुभवों में समभाव रख पाता हूँ?
- क्या मैं परमात्मा के अनुभव के लिए योग्य बना हूँ?
- क्या मैं वास्तव में अपने भीतर की चंचलता पर विजय पाने की साधना कर रहा हूँ?
निष्कर्ष
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण हमें यह बताना चाहते हैं कि ईश्वरप्राप्ति या आत्मसाक्षात्कार किसी विशेष पूजा-पद्धति, बाहरी आडंबर या कर्मकांड से नहीं होता — वह भीतर की साधना, मन की शांति, और द्वंद्वों से ऊपर उठने की अवस्था से प्राप्त होता है।
जितात्मा वही है जो अपने अंतःकरण को वासनाओं से मुक्त, इन्द्रियों पर नियंत्रण और चित्त को शांत करके, सभी अनुभवों में समभाव रखता है।
ऐसे योगी के लिए परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर स्थित और अनुभव योग्य होता है।
“जब चित्त स्थिर हो, मन शांत हो, इन्द्रियाँ संयमित हों — तब ही आत्मा परमात्मा को धारण कर सकती है।”
यह श्लोक गीता के योग, संतुलन और समत्व के दर्शन का सार है — जो हमें सिखाता है कि आत्मिक शांति और समत्व ही ब्रह्म को आत्मा में प्रकट करते हैं।
वास्तव में, परमात्मा बाहर कहीं नहीं — वह आत्मा में तभी समाहित होता है जब हम भीतर से तैयार होते हैं।
