मूल श्लोक – 1
श्रीभगवान उवाच —
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु॥
शब्दार्थ
| संस्कृत शब्द | हिन्दी अर्थ |
|---|---|
| श्रीभगवान उवाच | भगवान श्रीकृष्ण ने कहा |
| मयि | मुझमें (भगवान में) |
| आसक्त-मनाः | मन से आसक्त, पूर्ण प्रेम व लगाव रखने वाला |
| पार्थ | हे पार्थ! (अर्जुन) |
| योगं युञ्जन् | योग का अभ्यास करते हुए |
| मद-आश्रयः | मेरी शरण में रहकर, मुझ पर पूर्ण निर्भर होकर |
| असंशयम् | बिना किसी संदेह के |
| समग्रम् | पूर्ण रूप से, सम्पूर्ण रूप में |
| मां | मुझे (ईश्वर को) |
| यथा | जैसे, जिस प्रकार |
| ज्ञास्यसि | जान पाएगा, अनुभव करेगा |
| तत् | वह सब |
| शृणु | सुनो |
परम प्रभु ने कहा-हे अर्जुन! अब यह सुनो कि भक्तियोग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझमें अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो।
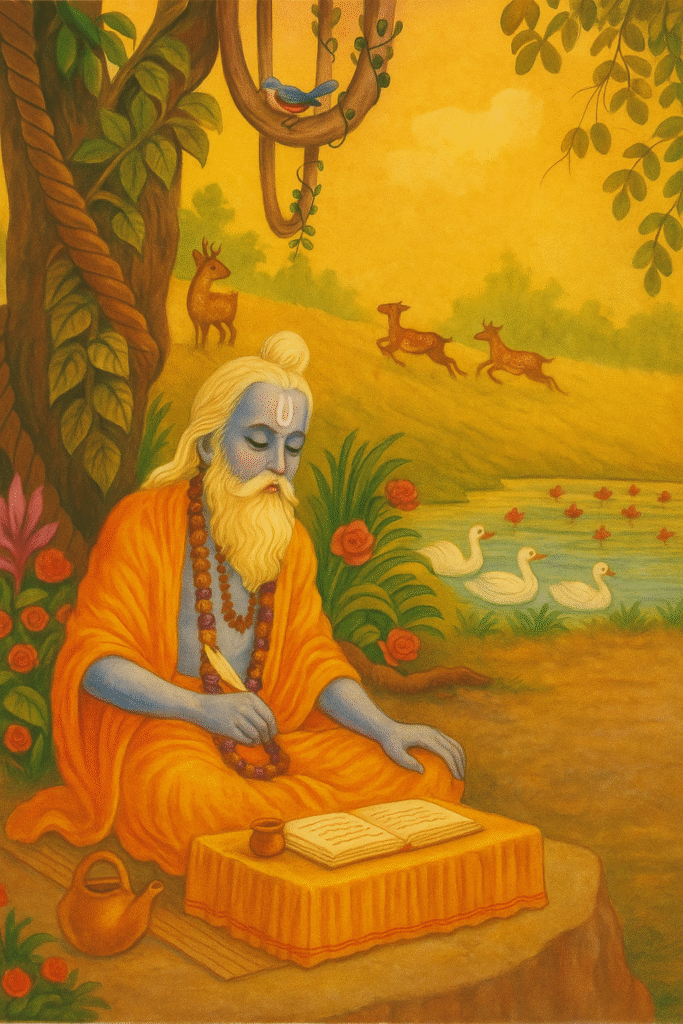
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक से भगवद्गीता का सातवाँ अध्याय “ज्ञान-विज्ञान योग” प्रारंभ होता है, जिसमें श्रीकृष्ण आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के संबंध में गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं।
श्रीकृष्ण यहाँ यह कह रहे हैं:
- जो साधक “मय्यासक्तमना” — मुझमें पूर्ण मन लगाकर, यानी प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से जुड़कर साधना करता है,
- और “मदाश्रयः” — मेरा ही आश्रय लेता है, न कि केवल अपने बल, ज्ञान या यंत्रणा पर निर्भर रहता है,
- और साथ ही “योगं युञ्जन्” — योग का नियमित अभ्यास करता है (ध्यान, भक्ति, आत्मसाक्षात्कार का प्रयास),
तो वह “असंशयं समग्रं मां ज्ञास्यसि” — निःसंदेह और सम्पूर्णता के साथ मुझे जान सकता है।
“तच्छृणु” — अब मैं तुझे यह रहस्य बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- यह श्लोक स्पष्ट करता है कि परमात्मा का ज्ञान केवल बुद्धि या युक्ति से नहीं, बल्कि आसक्ति (प्रेम), आश्रय (समर्पण) और योग (अनुभव) से संभव है।
- यहाँ “मय्यासक्तमना” शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है — केवल ईश्वर में भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि चित्त की संपूर्ण एकाग्रता भी।
- “मदाश्रयः” का अर्थ है — भगवान को ही गुरु, मार्गदर्शक, आधार और लक्ष्य मानना।
यह श्लोक बताता है कि ईश्वर का सच्चा ज्ञान — जो संदेहों से परे हो — केवल एक समर्पित योगी को ही प्राप्त होता है।
प्रतीकात्मक अर्थ
| शब्द | प्रतीकात्मक अर्थ |
|---|---|
| मय्यासक्तमना | ईश्वर में अनुरक्त, मन और चित्त से परमात्मा से जुड़ा हुआ |
| योगं युञ्जन् | जीवन को ध्यान, साधना, संयम और आत्म-अनुशासन से जोड़ना |
| मदाश्रयः | अपने समस्त कर्म, विचार और भावनाओं का केंद्र भगवान को बनाना |
| असंशयम् | पूर्ण विश्वास, जरा भी संदेह नहीं |
| समग्रम् | सम्पूर्ण ईश्वर — न केवल निराकार या साकार रूप में, बल्कि पूर्ण तत्त्वज्ञान में |
| तच्छृणु | अब इस गूढ़ ज्ञान को सुनने के लिए तैयार हो जाओ |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- ईश्वर को जानने के लिए भक्ति, योग और समर्पण की त्रयी अनिवार्य है।
- केवल शास्त्र पढ़कर ईश्वर को नहीं जाना जा सकता — इसके लिए आंतरिक अनुभूति और निष्ठा चाहिए।
- श्रीकृष्ण यह संकेत देते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर में मन को लगाकर, नियमित योग-साधना करता है, और आत्मा से उसे पकड़ लेता है, वही संदेहों से मुक्त होकर पूर्ण सत्य को जानता है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
- क्या मेरा मन वास्तव में ईश्वर में आसक्त है?
- क्या मैं योग को केवल अभ्यास मानता हूँ या ईश्वर से एकत्व की साधना समझता हूँ?
- क्या मैंने अपने जीवन में किसी के प्रति पूर्ण समर्पण का अनुभव किया है — जैसे श्रीकृष्ण यहाँ माँगते हैं?
- क्या मैं ईश्वर को “समग्र” रूप में जानने के लिए तत्पर हूँ — या केवल सुविधा अनुसार?
- क्या मैं संदेहों से परे जाकर श्रद्धा के साथ सुनने और जानने को तैयार हूँ?
निष्कर्ष
श्रीमद्भगवद्गीता के इस सातवें अध्याय का आरंभ ही एक अत्यंत गंभीर निमंत्रण से होता है —
“यदि तू सच्चे मन से मुझमें आसक्त हो, मुझ पर निर्भर हो, और योग का अभ्यास करे —
तो मैं तुझे सम्पूर्ण रूप से, संदेह से रहित होकर अपना ज्ञान दूँगा।”
यह श्लोक हमें आत्मा और परमात्मा के अनुभवात्मक संबंध की तैयारी के लिए आमंत्रित करता है।
अब गीता का ज्ञान केवल दर्शन नहीं, दिव्य साक्षात्कार की ओर बढ़ने वाला है।
आगे आने वाले श्लोकों में श्रीकृष्ण स्वयं को “ज्ञेय तत्त्व” के रूप में प्रकट करते हैं।
