मूल श्लोक: 48
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 48॥
शब्दार्थ
- योगस्थः — योग में स्थित होकर
- कुरु — करो
- कर्माणि — अपने कर्मों को
- सङ्गं त्यक्त्वा — आसक्ति का त्याग करके
- धनञ्जय — हे धन अर्जित करने वाले अर्जुन!
- सिद्धि-असिद्धयोः — सफलता और असफलता में
- समः भूत्वा — समभाव होकर
- समत्वं — समता, संतुलित दृष्टिकोण
- योगः उच्यते — उसे ही योग कहा गया है
हे अर्जुन! सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही समभाव योग कहलाता है।
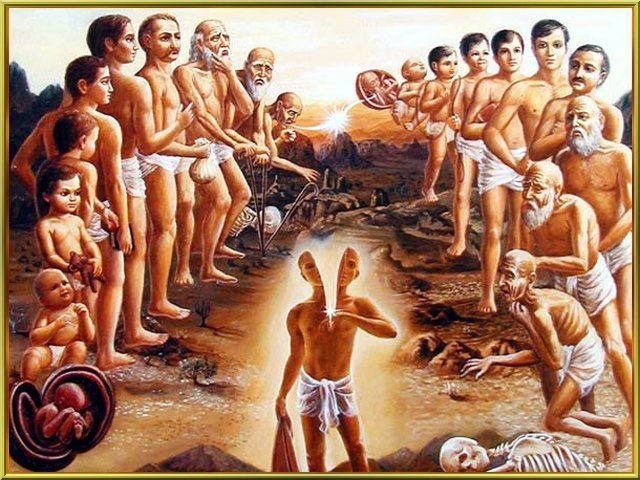
विस्तृत भावार्थ
श्रीकृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कर्मयोग का मर्म समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि:
- कर्म करना मनुष्य का धर्म है,
- किंतु कर्म के फल से आसक्ति रखना मोह है।
- जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्तव्य करता है और
- सफलता या असफलता में एक-सा रहता है, वही योगी कहलाता है।
यहां योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में समत्व बनाए रखना है।
भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण
1. ‘योगस्थः कुरु कर्माणि’ — योग में स्थित होकर कर्म करो
यहां ‘योगस्थः’ का तात्पर्य है – अंतर्मन से जुड़कर, स्थिर बुद्धि से कर्म करना। श्रीकृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को:
- ध्यानपूर्वक, विवेकपूर्ण, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए,
- ताकि वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित न हो,
- और अपने जीवन का ध्येय भूल न जाए।
योगस्थ होने का अर्थ है – अपने कर्तव्य में रत रहकर भी आत्मा में स्थित रहना।
2. ‘सङ्गं त्यक्त्वा’ — आसक्ति का त्याग करो
कर्म करते समय दो प्रकार की आसक्तियाँ होती हैं:
- कर्म की आसक्ति — “मैं यह काम करूं या न करूं?”,
- फल की आसक्ति — “मुझे इसका फल क्या मिलेगा?”
श्रीकृष्ण कहते हैं कि इन दोनों को त्याग दो। जब तक कर्म फल की आशा से किया जाता है, तब तक वह बंधनकारक होता है।
सच्चा योगी वह है जो कर्म को ईश्वरार्पण समझकर करता है।
3. ‘धनञ्जय’ — विशेष संबोधन
यहां अर्जुन को ‘धनञ्जय’ कहकर पुकारा गया है — जिसका अर्थ है “जो युद्ध में धन (विजय, वैभव) अर्जित करता है”। यह स्मरण दिलाता है कि तुम विजेता हो, अब यह विजय आत्मिक समता में होनी चाहिए, न केवल भौतिक युद्ध में।
4. ‘सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा’ — सफलता और असफलता में समभाव
सफलता या असफलता जीवन के परिणाम हैं। श्रीकृष्ण समझाते हैं कि:
- परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते।
- केवल कर्म करना हमारा अधिकार है।
- यदि हम फल में उलझते हैं, तो मन चंचल हो जाता है।
- लेकिन जब हम फल में समभाव रखते हैं, तो मानव जीवन की शांति और मुक्ति का द्वार खुलता है।
यह स्थिरबुद्धि योग की पहली पहचान है — राग-द्वेष से मुक्त समत्व।
5. ‘समत्वं योग उच्यते’ — समता ही योग है
यह श्लोक गीता के कर्मयोग दर्शन का मूल स्तंभ है।
‘योग’ शब्द का सामान्य अर्थ होता है – जोड़ना। यहाँ योग का अर्थ है:
- अपने कर्तव्य से जुड़ना,
- फल की चिंता से मुक्त होकर,
- आत्मा की स्थिति में स्थित होकर,
- हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखना।
समत्व ही सच्चा योग है। यह मन की तटस्थता, आत्मिक स्थिरता, और संतुलित दृष्टिकोण की अवस्था है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
यह श्लोक गीता का हृदय है — जिसमें श्रीकृष्ण मानव जीवन की उच्चतम साधना का सूत्र देते हैं:
- मनुष्य को कर्म तो करना है, परंतु फल के मोह में नहीं फँसना चाहिए।
- ‘योग’ कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और समत्व की अवस्था है।
- जीवन में जो कुछ भी हो — लाभ-हानि, जय-पराजय — यदि मन स्थिर रहता है, तो वही सच्ची साधना है।
यह विचार केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
प्रतीकात्मक अर्थ
- धनञ्जय — बाह्य विजय का प्रतीक, जिसे अब आंतरिक विजय प्राप्त करनी है
- कर्म — जीवन का अनिवार्य कर्तव्य
- सिद्धि-असिद्धि — संसार का द्वैत
- समत्व — जीवन की संतुलित दृष्टि
- योगस्थ — स्थिरबुद्धि आत्मज्ञानी
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा:
- जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, परंतु फल की चिंता छोड़ दो।
- सफलता या असफलता, दोनों को एक जैसा देखना ही सच्चा संतुलन है।
- योग कोई क्रिया नहीं, बल्कि मन की स्थिति है।
- कर्म करते हुए शांत रहना, यही ईश्वर से साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है।
- बुद्धिमत्ता वही है जो कर्म करता है पर बँधता नहीं।
आत्मचिंतन के प्रश्न:
क्या मैं अपने कर्मों को फल की अपेक्षा के साथ करता हूँ?
क्या मैं सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देख पाता हूँ?
क्या मेरा मन निरंतर चिंता, भय या अपेक्षा में फंसा रहता है?
क्या मैं अपने कर्तव्यों को ईश्वरार्पण की भावना से कर रहा हूँ?
क्या मैं योग के वास्तविक अर्थ — समत्व — को अपने जीवन में ला रहा हूँ?
निष्कर्ष (Conclusion):
इस श्लोक में श्रीकृष्ण ने हमें कर्मयोग का सार प्रदान किया है — कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त रहना, और हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखना।
यह न केवल आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है, बल्कि व्यवहारिक जीवन की कुशलता का भी रहस्य है।
जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है और परिणामों में समता रखता है, तभी वह सच्चा योगी बनता है। यही गीता का मधुर संदेश है — जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के रणभूमि में था।
