मूल श्लोक: 23
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥23॥
शब्दार्थ
- गतसङ्गस्य — जो सङ्ग से मुक्त हो चुका हो (सङ्गात् विमुक्त)।
- मुक्तस्य — जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, बन्धन रहित।
- ज्ञानावस्थितचेतसः — जिसका चित्त (मन) ज्ञान की स्थिर स्थिति में स्थित हो।
- यज्ञायाचरतः — जो अपने कर्म को यज्ञ के रूप में करता हो, अर्थात् निःस्वार्थ भाव से, ईश्वर को समर्पित कर।
- कर्म समग्रं प्रविलीयते — उसका सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाता है, या प्रवाहित होकर बंधन से मुक्त हो जाता है।
वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए सम्पन्न करते हैं और इसलिए वे कर्मफलों से मुक्त रहते हैं।
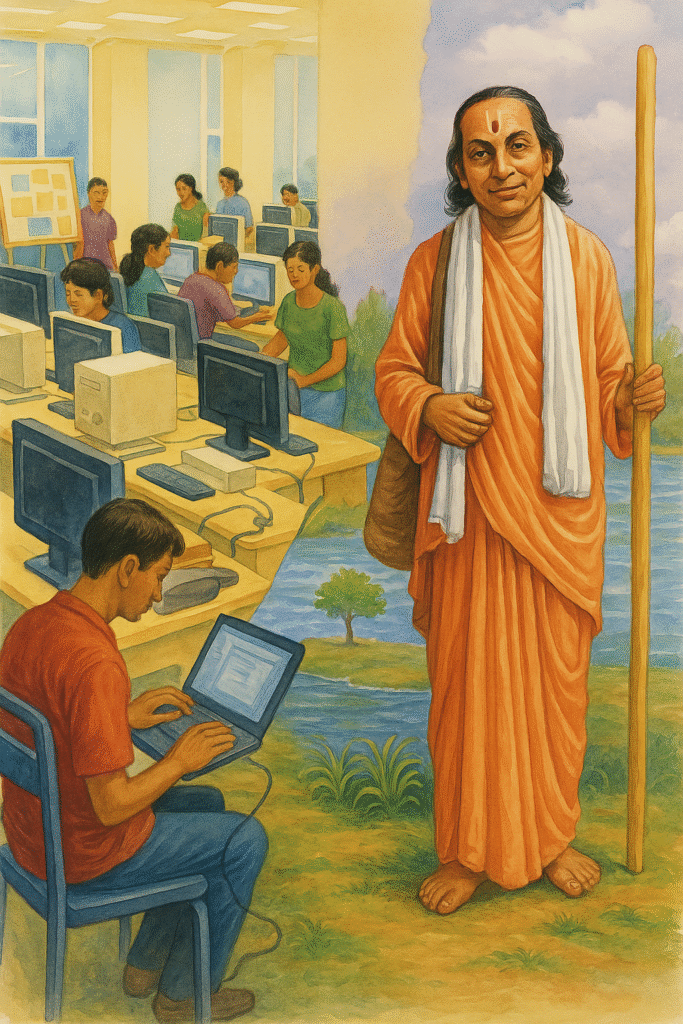
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण योग के परम सिद्धान्त को स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे एक ज्ञानी और मुक्त व्यक्ति के कर्मों का परिणाम उसे बाँधता नहीं है।
गतसङ्गस्य मुक्तस्य:
सङ्ग का अर्थ है आसक्ति, लगाव, या किसी वस्तु, व्यक्ति या फल की इच्छा। संसार में प्रायः कर्मों के साथ व्यक्ति का जुड़ाव रहता है। परन्तु जो व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका हो, अर्थात् जो अपनी इच्छाओं, संतान, संपत्ति, सुख-दुख आदि के प्रति आसक्त नहीं है, वही वास्तव में कर्मयोग में सफल होता है।
ज्ञानावस्थितचेतसः:
ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर होता है जो सत्य ज्ञान की गहराई को समझ चुका है। उसे अपने स्वभाव, आत्मा, परमात्मा और कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। उसका मन विचलित नहीं होता, न ही किसी भौतिक वस्तु में उलझा रहता है। यह ज्ञान उसके चित्त को स्थिरता और शान्ति प्रदान करता है।
यज्ञायाचरतः कर्म:
इस मुक्त, ज्ञानी व्यक्ति का कर्म भौतिक स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति यज्ञ के भाव से होता है। वह कर्म अपने अहंकार या फल की आशा के बिना करता है। कर्म को समर्पित भाव से करना उसे पवित्र बनाता है। कर्म अब उसका बोझ नहीं रह जाता बल्कि एक प्रकार का आत्म-समर्पण बन जाता है।
समग्रं प्रविलीयते:
ऐसे कर्मों का संपूर्ण प्रभाव प्रवाहित होकर समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म नष्ट हो जाता है, बल्कि कि कर्मफल के बन्धन कर्मयोगी को बाँध नहीं पाते। कर्म योगी के लिए मोक्ष के मार्ग का साधन बन जाते हैं। उसके कर्म बंधन का कारण नहीं, बल्कि मुक्तिदायक साधन हैं।
भावात्मक व्याख्या एवं गहन विश्लेषण
यह श्लोक कर्मयोग के अन्तःकरण का सार प्रस्तुत करता है। संसार में कर्म के साथ आसक्ति और फल की इच्छा का होना मनुष्य को जन्म-मृत्यु के चक्र में फँसाता है। परन्तु यदि व्यक्ति संसारिक आसक्तियों से मुक्त हो, अपने चित्त को उच्चतम ज्ञान की अवस्था में स्थापित करे और कर्म को निःस्वार्थ भाव से यज्ञ के रूप में अर्पित करे, तो उसके कर्म उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं।
यह स्थिति एक उच्चतम योगी की होती है, जो चाहे किसी भी प्रकार का कर्म करे, वह कर्म उसे पाप और पुनर्जन्म के बन्धन में नहीं बाँधता। कर्म की यह प्रवाहिनी अवस्था उसे शाश्वत शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- सङ्ग से मुक्ति:
सङ्ग, या आसक्ति, संसार के बंधनों की मूल जड़ है। कर्मयोग का मूल उद्देश्य ही इस सङ्ग से मुक्त होना है। जब मन, वासनाएँ, और लोभ समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा को शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है। - ज्ञान की स्थिरता:
ज्ञान केवल पांडित्य या पुस्तकज्ञान नहीं, बल्कि आत्म-स्वरूप के अनुभव और ईश्वरोपासना में निरंतरता है। चित्त का ज्ञान में स्थिर होना ही मोक्ष की प्राप्ति का आधार है। - यज्ञ के रूप में कर्म:
यह कर्म निःस्वार्थ होता है। कर्मफल की इच्छा त्याग कर कर्म करना कर्मयोग की सर्वोच्च अवस्था है। कर्म को ईश्वर को समर्पित यज्ञ मानना व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है। - कर्मों का प्रवाह:
जब यह सब गुण प्राप्त हो जाते हैं, तो कर्मों का प्रभाव प्रवाहित होकर समाप्त हो जाता है। कर्मयोगी के लिए कर्म बंधनकारी नहीं रह जाता।
प्रतीकात्मक अर्थ
| प्रतीक | अर्थ |
|---|---|
| गतसङ्गस्य | संसार के बंधनों और आसक्तियों से मुक्त होना |
| मुक्तस्य | पूर्ण स्वतंत्र, बन्धन रहित अवस्था |
| ज्ञानावस्थितचेतसः | चित्त का ज्ञान की स्थिर अवस्था में स्थित होना |
| यज्ञायाचरतः कर्म | कर्म को ईश्वर को अर्पित करने का भाव लेकर करना |
| समग्रं प्रविलीयते | कर्मों का प्रभाव समाप्त होकर बन्धन से मुक्त होना |
आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा
- संसारिक आसक्ति से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है।
- अपने मन को ज्ञान की स्थिर अवस्था में स्थापित करें।
- कर्म करते समय फल की इच्छा त्यागें और उसे ईश्वर को समर्पित करें।
- कर्म योग का यही स्वरूप व्यक्ति को जन्म-मृत्यु के बन्धनों से मुक्त करता है।
- निःस्वार्थ भाव से कर्म करने से मनुष्य शाश्वत शान्ति और मोक्ष प्राप्त करता है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मैं अपने कर्मों से आसक्ति या फल की इच्छा को त्याग पाया हूँ?
क्या मेरा मन स्थिर है और ज्ञान की उच्चतम अवस्था में है?
क्या मैं अपने कर्मों को यज्ञ के भाव से ईश्वर को अर्पित करता हूँ?
क्या मेरे कर्म मुझे बंधन में बाँधते हैं या वे मुक्ति के साधन बने हैं?
क्या मैं संसारिक लगाव से मुक्त होकर अपने कर्मों को करता हूँ?
निष्कर्ष
भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में योग के उस परम सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं, जिसमें संसार के बंधनों से मुक्त, ज्ञान में स्थिरचित्त योगी के कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के भाव से होते हैं। ऐसे योगी के कर्म उसके लिए बाधा नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। कर्म का समग्र प्रभाव प्रवाहित होकर समाप्त हो जाता है और योगी जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है।
यह श्लोक कर्मयोग के उच्चतम सिद्धांत को उद्घाटित करता है, जो हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी कैसे बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। यही ज्ञान, यही मुक्ति का मार्ग है।
