मूल श्लोक – 13
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन् ॥
शब्दार्थ (शब्दों का संक्षिप्त अर्थ)
- सर्वकर्माणि — सभी कर्मों को
- मनसा — मन द्वारा (भावना या चित्त से)
- संन्यस्य — त्यागकर, समर्पित करके
- आस्ते — स्थित रहता है, टिकता है
- सुखम् — सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक
- वशी — आत्मसंयमी, जिसने इन्द्रियों पर विजय पा ली है
- नवद्वारे पुरे — नौ द्वारों वाला नगर (मानव शरीर रूपी नगर)
- देही — embodied soul, शरीर में स्थित आत्मा
- नैव कुर्वन् — न स्वयं कुछ करता है
- न कारयन् — न दूसरों से कुछ कराता है
जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, नौ द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं क्योंकि वे स्वयं को कर्त्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं।
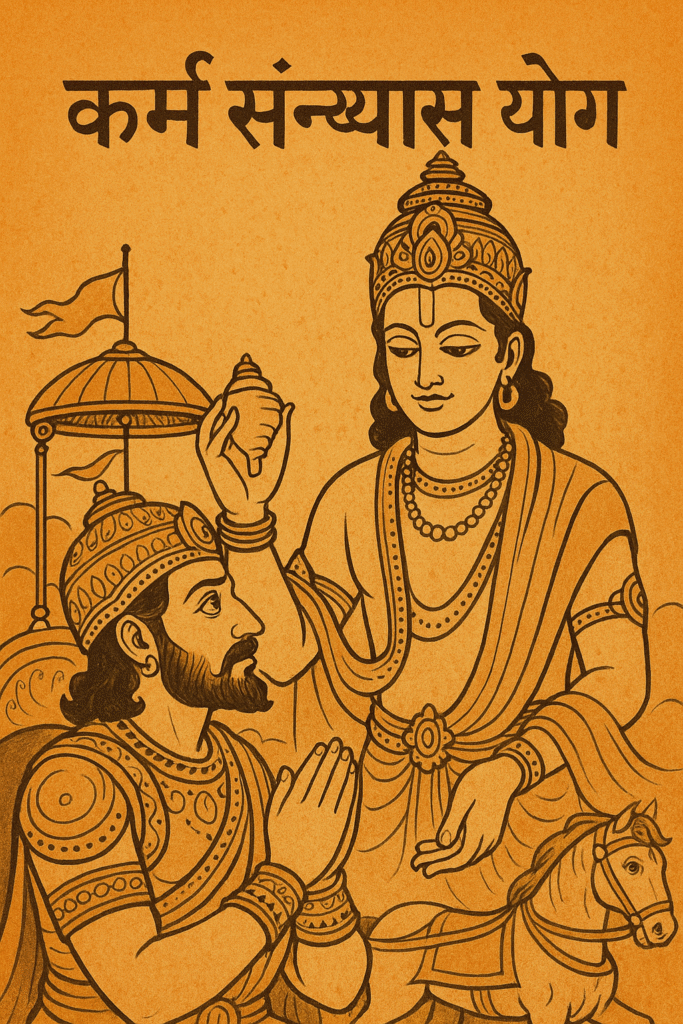
विस्तृत भावार्थ
यह श्लोक उस सिद्ध योगी की स्थिति का वर्णन करता है, जिसने बाह्य जगत में कर्म करते हुए भी आंतरिक रूप से सम्पूर्ण वैराग्य और समर्पण को प्राप्त कर लिया है। वह योगी सभी कर्मों को “मनसा संन्यस्य” — अर्थात् अंतःकरण से त्यागकर, परमात्मा को समर्पित करता है। वह बाह्य रूप से शरीर के कार्य होते हुए भी यह जानता है कि “मैं कर्ता नहीं हूँ।”
“नवद्वारे पुरे” — यह शरीर रूपी नगर को नौ द्वारों वाला कहा गया है, जो नौ इन्द्रिय-द्वारों (दो नेत्र, दो नासिका, दो कान, मुख, गुदा और मूत्रद्वार) से युक्त है। इस नगर में स्थित “देही” — आत्मा — केवल साक्षी है। आत्मसंयमी योगी इस साक्षीभाव में स्थित होकर, अपने को न कर्ता मानता है और न कर्म के फल से जुड़ता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- कर्तृत्व-अभाव (Non-doership): यह श्लोक गीता के कर्तापन के अभाव को रेखांकित करता है।
योगी जानता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं; आत्मा तो साक्षी मात्र है। - साक्षीभाव (Witness consciousness):
योगी शरीर में रहते हुए भी आत्मा के स्तर पर स्थित रहता है। न वह करता है, न करवाता है। - शुद्ध आत्मा की स्थिति:
आत्मा निष्क्रिय और निरपेक्ष है। यह शरीर और मन ही हैं जो कार्य करते हैं। - नवद्वार और आत्मा का प्रतीकात्मक सम्बंध:
शरीर रूपी नगर में आत्मा एक अव्यक्त, अविकार साक्षी के रूप में विद्यमान रहती है, जब वह योगी बन जाती है।
प्रतीकात्मक अर्थ
- सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य — समस्त कर्मों को अंतःकरण से त्याग देना, भगवान को समर्पित कर देना।
- वशी — जिसने मन, इन्द्रियाँ और अहंकार पर नियंत्रण पा लिया है।
- नवद्वारे पुरे — शरीर को एक नगर रूप में देखना, जहाँ आत्मा एक राजा की तरह स्थित है।
- देही — आत्मा जो इस शरीर में वास करती है।
- नैव कुर्वन् न कारयन् — आत्मा न स्वयं कर्म करती है, न दूसरों से करवाती है — यह सब प्रकृति के गुण करते हैं।
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- कर्तापन की भावना का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है।
– जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह कर्ता नहीं, केवल साक्षी है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। - शरीर में रहते हुए भी आत्मा स्वतंत्र रह सकती है।
– यही योग की अवस्था है — संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहना। - आत्मसंयम और वैराग्य ही शांति के मूल आधार हैं।
– जिसने इन्द्रियों को जीत लिया, वही सुखपूर्वक जी सकता है। - कर्म का बाह्य परित्याग नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण आवश्यक है।
– मन से संन्यास ही वास्तविक संन्यास है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मैं अपने कर्मों में “कर्तापन” की भावना रखता हूँ?
क्या मैं कर्म करते हुए उन्हें ईश्वर को समर्पित कर पाता हूँ?
क्या मैंने अपने शरीर और इन्द्रियों को संयमित किया है?
क्या मैं आत्मा को इस शरीर रूपी नगर का साक्षी मानता हूँ?
क्या मैं भीतर से शांत, संतुलित और अलिप्त रहकर कर्म कर सकता हूँ?
निष्कर्ष
यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चा योगी वह नहीं है जो संसार छोड़कर बैठ जाए, बल्कि वह है जो सभी कर्मों को मन से त्यागकर, ईश्वर को समर्पित करके, संयमपूर्वक, साक्षी भाव से संसार में स्थित रहता है।
नवद्वारों से युक्त यह शरीर एक नगर है और उसमें स्थित आत्मा एक साक्षी राजा है — जब यह ज्ञान प्रकट होता है, तब कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं।
गीता का यह अमृतवाक्य हमें कर्म के जाल से पार जाने का सरल और सूक्ष्म उपाय बताता है — त्याग और साक्षीभाव।
