मूल श्लोक – 27
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥
शब्दार्थ
| संस्कृत शब्द | हिन्दी अर्थ |
|---|---|
| इच्छा | आकर्षण, चाह, राग |
| द्वेष | घृणा, नापसंद, विरोध |
| समुत्थेन | उत्पन्न हुए, द्वारा उत्पन्न |
| द्वन्द्वमोहेन | द्वन्द्व रूपी मोह से, द्वैत के भ्रम से |
| भारत | हे भारतवंशी अर्जुन |
| सर्वभूतानि | सभी प्राणी |
| सम्मोहम् | मोह में, भ्रम में |
| सर्गे | सृष्टि के समय, जन्म के समय |
| यान्ति | चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं |
| परन्तप | हे शत्रुओं का दमन करने वाले (अर्जुन) |
हे भरतवंशी! इच्छा तथा घृणा के द्वन्द मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता! भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं।
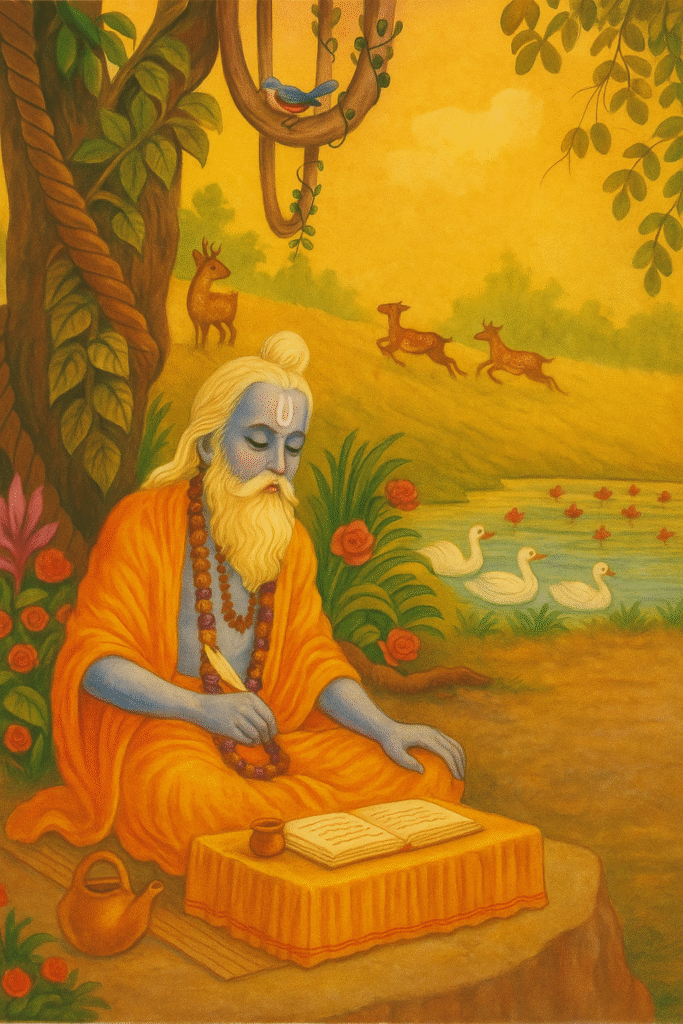
विस्तृत भावार्थ
भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब कोई जीव इस संसार में जन्म लेता है, तो वह पहले ही एक गहरे भ्रम में प्रवेश करता है। यह भ्रम केवल अज्ञान के कारण नहीं है, बल्कि इच्छा (राग) और द्वेष (द्वैत) से उत्पन्न होता है — जिसे शास्त्रीय भाषा में द्वन्द्व कहा गया है।
हर मनुष्य सुख को चाहता है और दुःख से घृणा करता है। यही इच्छा और द्वेष उसे मोह में डाल देती हैं। इस मोह के कारण जीव यह नहीं जान पाता कि वह वास्तव में कौन है, ईश्वर क्या हैं, और जीवन का उद्देश्य क्या है।
इस द्वन्द्व और मोह की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि सृष्टि के साथ ही यह सम्मोहन आरंभ हो जाता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है, उसी क्षण वह ‘मैं यह हूँ’, ‘मुझे यह चाहिए’, ‘मुझे इससे घृणा है’ जैसे भ्रमों में पड़ जाती है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
यह श्लोक अविद्या (अज्ञान) और द्वैतभाव की उत्पत्ति को समझाता है।
वेदांत के अनुसार, जब जीव ‘स्व’ से विमुख होकर ‘द्वैत’ (मैं और यह, सुख और दुःख, अच्छा और बुरा) की ओर आकर्षित होता है, तब ‘मोह’ उत्पन्न होता है।
इच्छा और द्वेष मन के दो पक्ष हैं — जहाँ इच्छा है, वहाँ द्वेष भी है। जहाँ राग है, वहाँ विराग भी। इस द्वैत के बीच झूलते हुए प्राणी जन्म-जन्मान्तर तक भ्रमित रहता है।
प्रतीकात्मक अर्थ
| शब्द / पंक्ति | प्रतीकात्मक अर्थ |
|---|---|
| इच्छा-द्वेष | मन की खिंचाव और विरोध की प्रवृत्तियाँ, राग-द्वेष |
| द्वन्द्वमोहेन | द्वैत के कारण उत्पन्न होने वाला आत्मविस्मृति का भ्रम |
| सर्गे यान्ति सम्मोहम् | जन्म लेते ही आत्मस्वरूप को भूल जाना |
| सर्वभूतानि | सभी जीव — कोई इससे अछूता नहीं |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- आत्मा जब शरीर लेती है, तभी से वह इच्छा-द्वेष की प्रवृत्तियों में फँस जाती है।
- यह द्वैत मनुष्य को सत्य से दूर करके संसार में भ्रमित करता है।
- जो साधक इच्छा और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है।
- मुक्तिपथ पर पहला कदम यही है कि हम अपने राग-द्वेष को पहचानें और उससे ऊपर उठें।
आत्मचिंतन के प्रश्न
- क्या मैं अपनी इच्छाओं और द्वेष के अधीन होकर निर्णय लेता हूँ?
- क्या मैं इस संसार को द्वैत रूप में देख रहा हूँ — सुख/दुःख, लाभ/हानि?
- क्या मेरी साधना मुझे मोह से बाहर निकाल रही है?
- क्या मैंने कभी विचार किया कि मेरा भ्रम सृष्टि के साथ ही क्यों शुरू होता है?
- क्या मैं अपने भीतर चल रहे ‘द्वन्द्व’ को शांत करने का प्रयास करता हूँ?
निष्कर्ष
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण आत्मा के जन्म के समय से ही प्रारंभ हो रहे अज्ञान, मोह और द्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं।
इच्छा और द्वेष — ये दो विपरीत ध्रुव व्यक्ति को सदा संसार के चक्र में बाँधे रखते हैं।
जब तक साधक इस द्वन्द्व से ऊपर नहीं उठता, तब तक आत्मसाक्षात्कार सम्भव नहीं।
अतः यह श्लोक ज्ञान और वैराग्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है — ताकि जन्म-जन्मांतर से चल रही यह सम्मोहन की श्रृंखला समाप्त हो और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर उन्मुख हो।
सच में मुक्त वही है, जो द्वन्द्व से मुक्त है।
और ज्ञानी वही है, जो इच्छा-द्वेष को पीछे छोड़कर आत्मा की ओर उन्मुख होता है।
