मूल श्लोक: 47
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 47॥
शब्दार्थ (शब्दों का अर्थ):
- कर्मणि एव अधिकारः ते — तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है
- मा फलेषु कदाचन — फल में कभी मत रखो (अपेक्षा मत करो)
- मा कर्मफलहेतुर्भूः — कर्म के फल की प्राप्ति को ही अपना कारण मत मानो
- मा ते सङ्गः अस्तु अकर्मणि — तुझे अकर्म (कर्म न करने) में भी आसक्ति न हो
तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है लेकिन अपने कर्मों के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं हे, तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो।
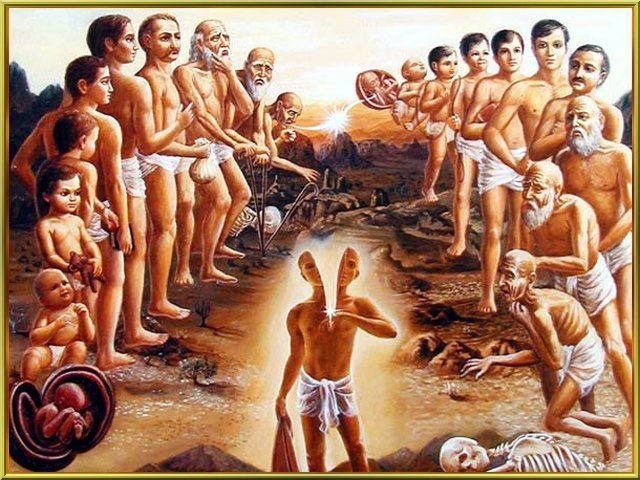
विस्तृत भावार्थ:
भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में कर्मयोग की मूलभूत शिक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है — लेकिन वह कर्म से उत्पन्न होने वाले फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यदि हम फल की चिंता करके कर्म करें, तो हमारी मन:स्थिति अशांत हो जाती है, और अपेक्षा, मोह, क्रोध, निराशा आदि भाव उत्पन्न होते हैं।
इसलिए श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय निष्काम भाव रखें — यानी कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म ही न करें (अकर्म) — क्योंकि कर्म से भागना भी मोह है।
भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण
क. “कर्मण्येवाधिकारस्ते” — तेरा अधिकार केवल कर्म पर है
श्रीकृष्ण यहां यह स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, न कि उसके परिणाम को नियंत्रित करने का। यह संसार कारण और परिणाम (Cause and Effect) के नियमों से चलता है, लेकिन हर परिणाम अनेक कारकों से बनता है — जैसे समय, स्थान, दूसरे लोग, प्रकृति आदि। हम केवल अपना कर्म नियंत्रित कर सकते हैं, फल नहीं।
यह विचार अहंकार को समाप्त करता है, क्योंकि फल को अपना समझना ही अहंकार है।
ख. “मा फलेषु कदाचन” — कभी भी फल की अपेक्षा मत रखो
जब हम किसी कार्य को करते समय फल की आशा से बंध जाते हैं, तो हमारी एकाग्रता बँट जाती है — न तो कर्म पूर्ण होता है, न ही शांति मिलती है। श्रीकृष्ण यह शिक्षा देते हैं कि फल पर अधिकार नहीं है, इसलिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
फल की चिंता करने से भय, लोभ और निराशा जैसी भावनाएँ पैदा होती हैं। निष्काम कर्म करने से मन स्थिर रहता है।
ग. “मा कर्मफलहेतुर्भूः” — कर्म का हेतु केवल फल न हो
यहाँ श्रीकृष्ण एक गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की ओर संकेत करते हैं — यदि हम कर्म को केवल फल के लिए करें, तो वह स्वार्थ हो जाता है। स्वार्थजनित कर्म bondage (बंधन) लाता है। ऐसे कर्म में मनुष्य स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि फल की प्राप्ति का दास बन जाता है।
जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब वह कर्म योग बन जाता है, और हमें कर्म के बंधन से मुक्त करता है।
घ. “मा ते सङ्गः अस्तु अकर्मणि” — कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो
कई लोग सोचते हैं कि यदि फल की अपेक्षा नहीं रखनी, तो फिर कर्म क्यों करें? ऐसे विचार से वे कर्म से भागने लगते हैं। श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं — अकर्म, यानी कि कोई कर्म न करना, एक प्रकार का मोह है, एक प्रकार की भीरुता।
जो व्यक्ति कहता है, “मैं फल की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए कुछ नहीं करूँगा,” वह भी फल के कारण ही कर्म छोड़ रहा है। यह भी एक प्रकार की आसक्ति है।
दार्शनिक दृष्टिकोण:
इस श्लोक में भगवद्गीता का केंद्रीय दर्शन समाहित है — कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह विचार उपनिषदों और योगदर्शन के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण मानव जीवन की सबसे बड़ी उलझन का समाधान दे रहे हैं — कर्म कैसे करें कि वह बंधन न बने?
उत्तर है: निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म का अर्थ है —
- कर्म पूरी श्रद्धा, निष्ठा और पूर्णता से करना
- फल की अपेक्षा को भगवान पर छोड़ देना
- कर्म को सेवा, भक्ति या धर्म का रूप देना
प्रतीकात्मक अर्थ:
- कर्म = जीवन का कर्तव्य
- फल = संसारिक अपेक्षाएँ
- अधिकार = कर्म करने की स्वतंत्रता
- अकर्म = पलायन, निष्क्रियता, आलस्य
- संग = मोह, आसक्ति
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा:
- कर्म करते समय फल की अपेक्षा न रखें, केवल समर्पण भाव रखें
- जीवन में कार्य करते हुए संतुलन और मानसिक शांति बनाए रखें
- परिणाम ईश्वर के अधीन हैं, हमारी भूमिका केवल साधन की है
- सफलता और असफलता के भाव से ऊपर उठें
- आलस्य और निष्क्रियता का कोई स्थान नहीं है — कर्म ही धर्म है
आत्मचिंतन के प्रश्न:
क्या मैं हर कार्य को फल की अपेक्षा से जोड़कर करता हूँ?
क्या मैं असफलता के भय से कर्म से भागता हूँ?
क्या मैं निष्काम भाव से सेवा करने की क्षमता रखता हूँ?
क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य को कर्म और धर्म के साथ जोड़ पाया हूँ?
क्या मैं कर्म करते हुए भगवान को समर्पण कर पाता हूँ?
निष्कर्ष:
यह श्लोक केवल एक कर्मसूत्र नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। श्रीकृष्ण कहते हैं —
- कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो
- कर्म करो, लेकिन फल पाने के लिए नहीं
- कर्म करो, लेकिन निष्क्रिय मत बनो
यह कर्मयोग का मूल मंत्र है। ऐसा कर्म योग में बदल जाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम हर कर्म को सेवा, समर्पण और भक्ति के रूप में करते हैं, तब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं।
