मूल श्लोक: 17
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥
शब्दार्थ
- कर्मणः — कर्म (action)
- हि अपि — निश्चय ही, भी
- बोद्धव्यं — जानना चाहिए, समझना चाहिए
- विकर्मणः — विकर्म (वर्ज्य कर्म या अनुचित कर्म)
- अकर्मणः — अकर्म (कर्म का न किया जाना, या निष्क्रियता)
- गहना — अत्यंत जटिल, रहस्यमय
- कर्मणः गतिः — कर्म की गति, कर्म का मार्ग, कर्म का परिणाम
तुम्हें सभी तीन कर्मों-कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनके सत्य को समझना कठिन है।इनका ज्ञान गलत है।
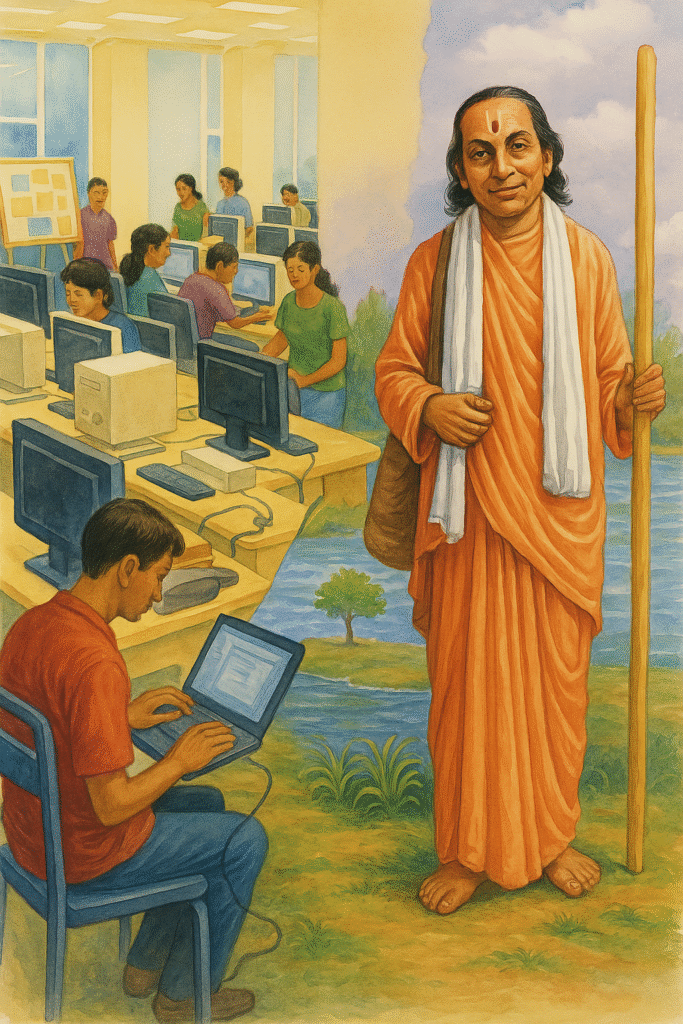
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म के तीन प्रमुख पहलुओं को समझने की प्रेरणा देते हैं:
- कर्म (सद्कर्म)
- वह कार्य जो धर्मानुसार और शास्त्रों के अनुसार हो।
- जैसे यज्ञ, दान, तप, सेवा, कर्तव्य पालन इत्यादि।
- विकर्म (दुष्कर्म)
- अधर्मजन्य, वर्ज्य, या नैतिक-अनैतिक कर्म।
- जैसे हिंसा, चोरी, अन्याय, लोभ आदि प्रेरित कार्य।
- अकर्म (निष्क्रियता या कर्म में कर्म का न दिखना)
- या तो कोई बाह्य क्रिया न करना (शरीरिक निष्क्रियता),
- या फिर ऐसा कर्म जिसमें बाह्य रूप से कर्म हो लेकिन वास्तव में वह “कर्म से मुक्त” हो — क्योंकि वह आसक्ति व फल की इच्छा रहित है।
श्रीकृष्ण कहते हैं कि ये तीनों आयाम अत्यंत गूढ़ हैं। केवल सतही ज्ञान से यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा कर्म उत्तम है और कौनसा अधम।
भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण
कर्म का महत्व और भ्रम
- सामान्यतः लोग मानते हैं कि कोई भी कार्य कर लेना ही ‘कर्म’ है, परंतु श्रीकृष्ण यहां बताते हैं कि हर कर्म का एक गूढ़ प्रभाव और परिणाम होता है।
- एक ही कार्य दो लोगों द्वारा किया गया, लेकिन उनके भाव, हेतु और दृष्टिकोण भिन्न होने पर उसका फल भी अलग हो सकता है। उदाहरण: एक सैनिक युद्ध करता है और एक डाकू भी हत्या करता है — लेकिन एक धर्म के लिए, दूसरा स्वार्थ के लिए। दोनों कर्म दिखते एक जैसे हैं, पर परिणाम और आत्मिक फल अलग।
विकर्म — चेतावनी का संकेत
- विकर्म वह है जो शास्त्रों द्वारा वर्जित है। यह व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाता है।
- विकर्म का परिणाम केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक पतन भी है।
- इसमें अहंकार, लालच, क्रोध आदि शामिल होते हैं।
अकर्म — परम रहस्य
- गीता में अकर्म का अर्थ केवल ‘कुछ न करना’ नहीं है।
- बल्कि ऐसा कर्म जो पूर्णतया निष्काम भाव से, ईश्वर को अर्पित करके किया गया हो — वह भी ‘अकर्म’ कहलाता है।
- बाह्य रूप से कर्म हो रहा है, लेकिन भीतर कोई ‘कर्तापन’ नहीं — यही अकर्म है।
यह योग की चरम स्थिति है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- कर्म की गति को केवल तर्क या सतही समझ से नहीं जाना जा सकता।
- गीता कहती है कि कर्म के परिणाम सिर्फ वर्तमान जन्म में ही नहीं, बल्कि भविष्य और अगली योनियों तक फैल सकते हैं।
- कर्म का दर्शन केवल क्रिया नहीं, बल्कि हेतु, भाव, नियत उद्देश्य, और असंगता पर आधारित है।
प्रतीकात्मक अर्थ
| तत्व | प्रतीक | अर्थ |
|---|---|---|
| कर्म | दायित्व | धर्म और उद्देश्य से युक्त कार्य |
| विकर्म | विकृति | लोभ, मोह या अहं से प्रेरित कार्य |
| अकर्म | तात्त्विक योग | जो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं डालता |
| गहना | रहस्य | केवल बाह्य बुद्धि से नहीं, अंतर्दृष्टि से समझना संभव |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- हर कर्म का मूल्यांकन करें
- सिर्फ “क्या किया?” नहीं, बल्कि “क्यों किया?”, “कैसे किया?”, और “किसके लिए किया?” को भी देखिए।
- विचारशील कर्म आवश्यक
- बिना सोचे कर्म करना या परंपरा के नाम पर कुछ करना ही सही नहीं। विवेक और ज्ञान आवश्यक है।
- निष्काम कर्म ही अकर्म है
- जब कोई व्यक्ति फल की आकांक्षा और ‘मैं कर रहा हूँ’ के अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है, तभी वह बंधन से मुक्त होता है।
- विकर्म से बचो, अकर्म की ओर बढ़ो
- आत्मनिरीक्षण करें कि कहीं हमारे कर्म विकर्म की श्रेणी में तो नहीं आ रहे?
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मैं कर्म का अर्थ केवल बाहरी क्रिया में समझता हूँ?
क्या मेरे जीवन में कुछ विकर्म हैं जिनसे मुझे सचेत होने की आवश्यकता है?
क्या मैं वास्तव में अकर्म (निष्काम भाव) से कर्म कर पाता हूँ?
क्या मेरे कर्म मुझे बंधन में डाल रहे हैं या मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं?
क्या मैं कर्म के साथ उसका गूढ़ तात्त्विक ज्ञान भी प्राप्त कर रहा हूँ?
निष्कर्ष
भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में कर्म की गहनता को रेखांकित करते हैं। वे केवल कर्म करने की बात नहीं करते, बल्कि उसे समझने की आवश्यकता पर बल देते हैं।
कर्म, विकर्म और अकर्म — तीनों का विवेकपूर्वक अध्ययन आवश्यक है।
जिस प्रकार एक जहाज समुद्र की गहराइयों को बिना ज्ञान के पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवनरूपी सागर को पार नहीं कर सकता यदि वह कर्म की गहराई को न समझे।
यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं — उसे समझना, विवेचना करना और अंततः उसे परमात्मा को समर्पित करना ही वास्तविक कर्मयोग है।
