मूल श्लोक: 26
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥
शब्दार्थ
- श्रोत्र-आदीनि — कान आदि (श्रवण आदि)
- इन्द्रियाणि — इन्द्रियाँ
- अन्ये — अन्य लोग (भक्त, योगी)
- संयम-अग्निषु — संयम की अग्नियों में
- जुह्वति — होम करते हैं, अर्पण करते हैं
- शब्द-आदीन् — शब्द आदि (इन्द्रिय विषय)
- विषयान् — विषयों को (जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध)
- इन्द्रिय-अग्निषु — इन्द्रिय रूपी अग्नियों में
कुछ योगीजन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इन्द्रियों को संयमरूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इन्द्रियों के अन्य विषयों को इन्द्रियों के अग्निरूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं।
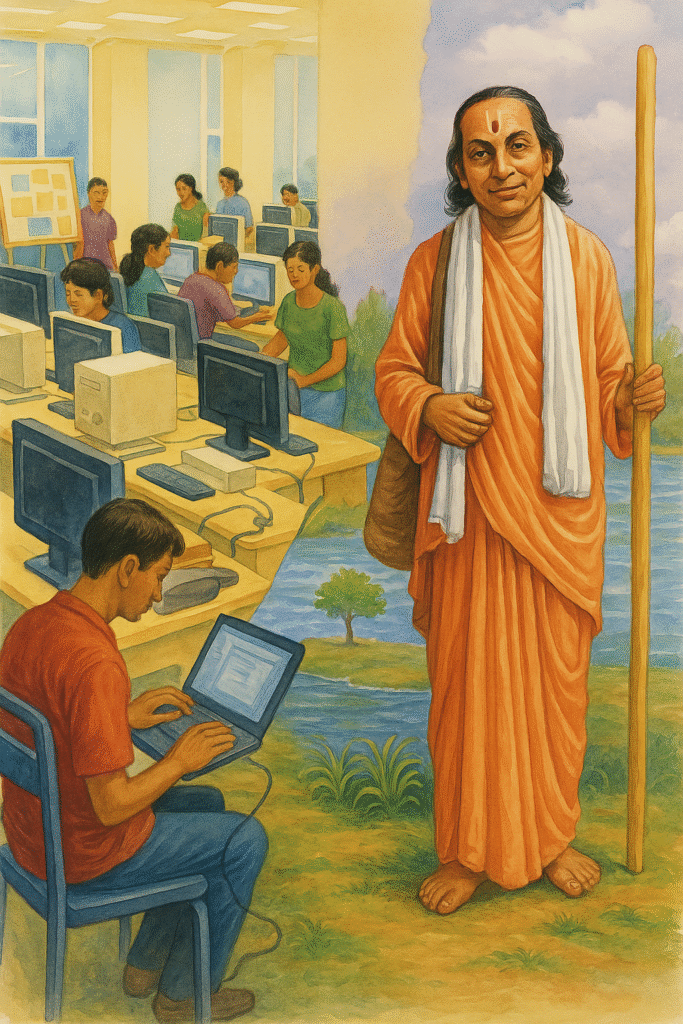
विस्तृत भावार्थ
यह श्लोक दो प्रकार की साधना का वर्णन करता है:
- इन्द्रिय-निग्रह की साधना
- इन्द्रिय-विषयों का यज्ञ रूप में समर्पण
पहले प्रकार में साधक अपनी इन्द्रियों को संयम (नियंत्रण) की अग्नि में होम करता है, अर्थात वह इन्द्रियों को विषयों से खींच लेता है और उन्हें भीतर की ओर मोड़ता है। यह ‘प्रत्याहार’ की स्थिति है, जहाँ योगी मन और इन्द्रियों को संयमित करता है।
दूसरे प्रकार में साधक अपनी इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने देता है, लेकिन वह इस भोग को भी एक यज्ञ बना देता है। यानी विषयों में लिप्त रहते हुए भी, वह आसक्ति से मुक्त रहता है और फल की कामना नहीं करता। उसकी यह वृत्ति भी त्याग और भक्ति से पूर्ण होती है।
भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण
दार्शनिक दृष्टिकोण
भगवद्गीता के अनुसार कोई भी कर्म — यदि वह समर्पण, त्याग और ईश्वर के प्रति निष्ठा से किया जाए — तो वह यज्ञ बन जाता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि किसी भी इन्द्रिय-वृत्ति का आत्म-नियंत्रण या ईश्वर को समर्पण करना भी यज्ञ है।
‘संयम-अग्नि’ का अर्थ है — आत्म-नियंत्रण की वह शक्ति जिसमें साधक अपनी इन्द्रियों को रोककर आत्मा में स्थिर करता है।
‘इन्द्रिय-अग्नि’ में विषय होम करना — इसका तात्पर्य यह है कि विषयों के माध्यम से भोग करने वाले योगी, अपनी तृप्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करते हैं, जिससे वह कर्म उन्हें बाँधता नहीं।
प्रतीकात्मक अर्थ
- श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ — श्रवण, दर्शन, स्पर्श, स्वाद और गंध की इन्द्रियाँ
- संयमाग्नि — आत्म-संयम, नियम, साधना की अग्नि
- इन्द्रियाग्नि — इन्द्रियों की प्रवृत्तियाँ, जो विषयों को ग्रहण करती हैं
- शब्दादि विषय — रूप, रस, गंध आदि संसारिक भोग के साधन
यहाँ अग्नि केवल यज्ञ की प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रेरणा, संवेदना, अहंकार और इच्छा की ऊर्जा का भी प्रतीक है।
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- संयम और भोग — दोनों ही यदि शुद्ध चित्त से किया जाएँ तो मोक्ष की दिशा में सहायक हो सकते हैं।
- आत्मसंयम की साधना कठिन है, परन्तु अत्यंत फलदायक है।
- इन्द्रियों का विषयों से संपर्क यदि लोभ, मोह और वासनाओं से मुक्त हो — तो वह भी यज्ञ बन सकता है।
- भगवान श्रीकृष्ण यहाँ विविध साधकों की प्रकृति का सम्मान करते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार साधना करता है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मैं अपनी इन्द्रियों को संयमित करने का प्रयास करता हूँ?
क्या मेरी विषयों के प्रति आसक्ति मुझे बाँधती है या मैं उसमें भी ईश्वरभाव देख पाता हूँ?
क्या मैं इन्द्रिय-संयम के यज्ञ में भाग ले रहा हूँ?
क्या मैं अपने कर्मों और भोगों को भी ईश्वर को अर्पित कर पाता हूँ?
निष्कर्ष
यह श्लोक यह सिखाता है कि साधना का मार्ग केवल एक नहीं होता। कुछ साधक इन्द्रियों को संयम की अग्नि में होम करते हैं, कुछ विषयों का भोग करते हुए भी उन्हें इन्द्रियाग्नि में समर्पित करते हैं — और यह दोनों ही यज्ञस्वरूप हैं।
मुख्य तत्व है — भाव, समर्पण और आसक्ति से मुक्ति।
भगवद्गीता का यह संदेश है कि कोई भी जीवन-प्रवृत्ति — यदि ईश्वर के प्रति समर्पण से की जाए — तो वह मोक्ष का साधन बन सकती है। संयम हो या भोग, यदि वह ‘यज्ञ’ बन जाए, तो साधक बंधन से मुक्त हो जाता है।
जीवन की हर क्रिया — देखना, सुनना, बोलना, स्वाद लेना — यदि ध्यान और समर्पण से की जाए तो वही साधना बन जाती है। यही गीता का यथार्थ और उपनिषदों की गूढ़ता है।
