मूल श्लोक – 12
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥12॥
शब्दार्थ:
- युक्तः — योगयुक्त व्यक्ति, आत्मसाक्षी योगी
- कर्मफलं त्यक्त्वा — कर्म के फल का त्याग करके
- शान्तिम् — परम शांति
- आप्नोति — प्राप्त करता है
- नैष्ठिकीम् — स्थायी, दृढ़, आध्यात्मिक शांति
- अयुक्तः — अयुक्त व्यक्ति, असंयमी, अनासक्त न होने वाला
- कामकारेण — कामना के वशीभूत होकर
- फले — फल में
- सक्तः — आसक्त, लिप्त
- निबध्यते — बंधता है, बंधन में पड़ता है
कर्मयोगी अपने समस्त कमर्फलों को भगवान को अर्पित कर परम शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामनायुक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वे बंधनों में पड़ जाते हैं क्योंकि वे कमर्फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं।
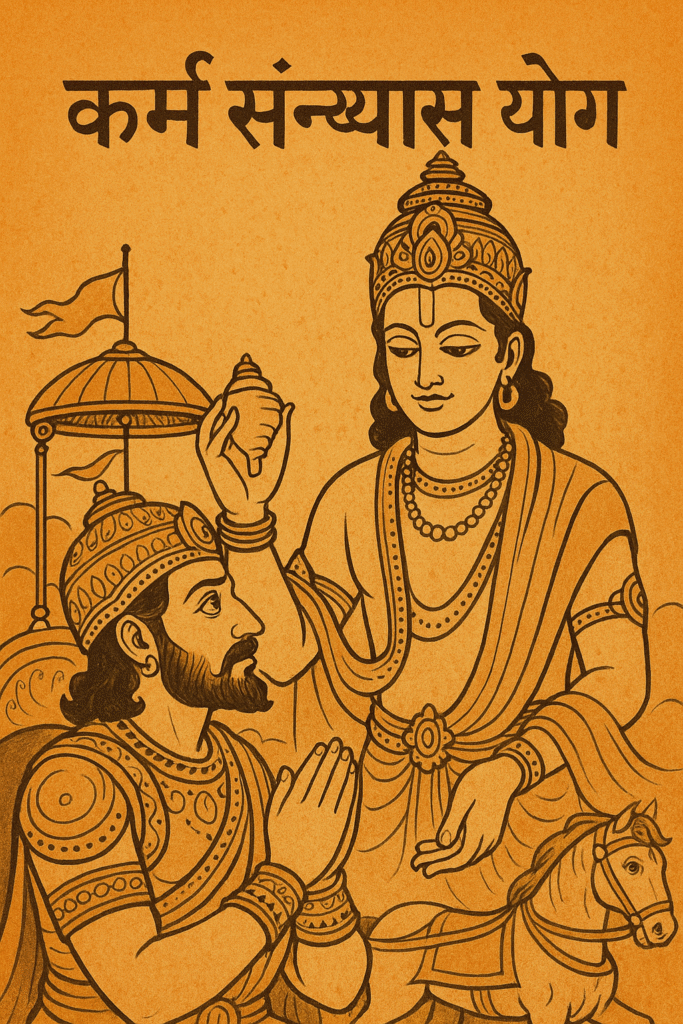
विस्तृत भावार्थ:
यह श्लोक कर्मफल के प्रति दृष्टिकोण के दो विपरीत पहलुओं को स्पष्ट करता है।
- युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा — यहाँ “युक्त” का अर्थ है – वह व्यक्ति जो योग में स्थिर है, जो आत्मज्ञानी है, और जिसकी बुद्धि समत्व में स्थित है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, परंतु उसका लक्ष्य केवल कर्तव्य-पालन होता है, फल की प्राप्ति नहीं। वह हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता।
- शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् — यह शांति केवल मन की सामान्य शांति नहीं है, बल्कि यह परमात्मा से एकत्व की शांति है — आत्मा की स्थिरता और संतुलन। यह “नैष्ठिकी” शांति है — जो अडिग, स्थायी और आध्यात्मिक है।
- अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः — जो व्यक्ति संयम से रहित है, और कर्म के फल में आसक्त रहता है, वह अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के कारण बार-बार जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है। उसका कर्म केवल स्वार्थ से प्रेरित होता है, जिससे वह पाप-पुण्य और सुख-दुख के चक्र में फँसता है।
- निबध्यते — फल की आकांक्षा मन में राग उत्पन्न करती है, राग से मोह, मोह से क्रोध, और फिर कर्मबंधन। यही बंधन आत्मा को संसार में बाँधता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण:
- कर्म और फल का योगदृष्टिकोण — गीता का मूल दर्शन यही है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की चिंता त्याज्य है।
- युक्त vs. अयुक्त — युक्त व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और ज्ञान से जोड़ता है। अयुक्त व्यक्ति अहंकार, इच्छाओं और अस्थिरता से ग्रस्त रहता है।
- शांति का मार्ग — शांति भोग से नहीं, त्याग से मिलती है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला ही अंततः मोक्ष और शांति प्राप्त करता है।
- बंधन की उत्पत्ति — जब कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, तो वह कर्म नहीं, व्यापार बन जाता है, जिससे आत्मा संसार के नियमों में बंध जाती है।
प्रतीकात्मक अर्थ:
- युक्तः — वह जो अपने मन, इंद्रियाँ और बुद्धि को संयमित कर चुका है
- कर्मफल त्याग — अपने हर कार्य का परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना
- नैष्ठिकी शांति — आत्मा की गहराई से उत्पन्न अडिग और परम शांति
- कामकारेण — इच्छाओं की दासता में किया गया कर्म
- निबद्धता — आत्मा की वह स्थिति जो उसे बार-बार बंधन और कष्ट में डालती है
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा:
- कर्तव्य भाव से कर्म करें, स्वार्थ भाव से नहीं
- फल की चिंता त्याग दें, क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है
- मन को संयमित करें और ईश्वर से जुड़कर कर्म करें
- कामना के अधीन कर्म पाप और बंधन को जन्म देता है
- सच्ची शांति केवल त्याग और समर्पण से मिलती है, नहीं कि इच्छा पूरी होने से
आत्मचिंतन के प्रश्न:
क्या मैं अपने जीवन के कर्म निष्काम भाव से करता हूँ या फल की अपेक्षा से?
क्या मेरी आंतरिक शांति परिस्थितियों पर निर्भर है या आत्मज्ञान पर?
क्या मैं कर्म में समत्व रखता हूँ या परिणाम से प्रभावित होता हूँ?
क्या मैं इच्छाओं के अधीन होकर कर्म करता हूँ?
क्या मैं आत्मा की नैष्ठिकी शांति की ओर अग्रसर हूँ या भौतिक इच्छाओं में बंधा हूँ?
निष्कर्ष:
भगवद्गीता का यह श्लोक हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जीवन में स्थायी शांति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति कर्म करता हुआ भी फल की आसक्ति से मुक्त होता है, तब वह नैष्ठिकी शांति — वह दिव्य, अचल, और पूर्ण आत्मिक शांति प्राप्त करता है।
इसके विपरीत, जब हम कर्म को इच्छाओं के अधीन करते हैं और फल की लालसा में उलझते हैं, तब हम बंधन के चक्र में फँसते हैं।
इसलिए, जीवन का आदर्श है – कर्म करो, पर फल की चिंता त्याग दो। यही मार्ग है शांति और मुक्ति का।
यह श्लोक हमें भीतर से हल्का और मुक्त जीवन जीने का मार्ग सिखाता है — आत्मा को कर्म में डुबोए बिना कर्म करते रहो।
