मूल श्लोक 4
साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥4॥
शब्दार्थ:
- साङ्ख्ययोगौ — सांख्य और योग (ज्ञानयोग और कर्मयोग)
- पृथक् — अलग-अलग
- बालाः — बालबुद्धि वाले, अपरिपक्व लोग
- प्रवदन्ति — कहते हैं
- न पण्डिताः — ज्ञानी लोग ऐसा नहीं कहते
- एकम् अपि — किसी एक का भी
- आस्थितः — ठीक प्रकार से स्थित रहने वाला
- सम्यक् — ठीक से, यथावत
- उभयोः — दोनों का
- विन्दते — प्राप्त करता है
- फलम् — फल
केवल अज्ञानी ही ‘सांख्य’ या ‘कर्म संन्यास’ को कर्मयोग से भिन्न कहते हैं जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे यह कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं।
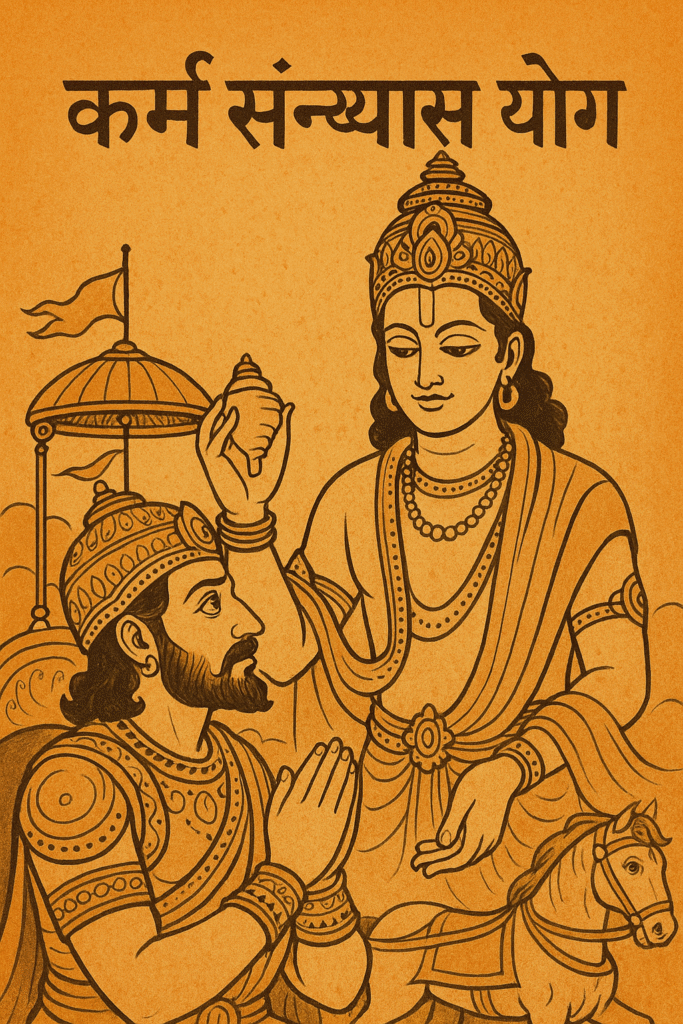
विस्तृत भावार्थ:
यह श्लोक भगवद्गीता के कर्म संन्यास योग (पंचम अध्याय) में आता है, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि आत्म-साक्षात्कार के दो मार्गों — ज्ञानयोग (सांख्य) और कर्मयोग (कर्म में स्थित रहकर निष्काम भाव से कार्य करना) — में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।
केवल वे लोग जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई नहीं है, जो सतही समझ रखते हैं, वे ही इन दोनों को अलग-अलग समझते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, वे इन दोनों को एक ही परम लक्ष्य की ओर अग्रसर मार्ग मानते हैं।
इस श्लोक में श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति ज्ञानमार्ग को अपनाए या कर्ममार्ग को, यदि वह उसमें दृढ़ है और सम्यक रीति से उसका पालन करता है, तो वह मोक्ष रूपी एक ही फल को प्राप्त करता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण:
- सांख्य और योग — सांख्य दर्शन का उद्देश्य है आत्मा और शरीर (प्रकृति) का भेद जानकर आत्मा की स्वतंत्रता को समझना। योग का उद्देश्य है मन को नियंत्रित कर आत्मा की स्थिति में स्थित होना। दोनों का लक्ष्य एक ही है — मोक्ष या आत्मबोध।
- ज्ञान और कर्म में समता — यह श्लोक यह संकेत करता है कि ज्ञान (विवेक) और कर्म (कर्मयोग) वास्तव में अलग नहीं हैं, बल्कि परस्पर पूरक हैं। ज्ञान के बिना कर्म बंधन देता है, और कर्म के बिना ज्ञान केवल सैद्धांतिक रह जाता है।
- ज्ञानी का दृष्टिकोण — जो तत्वदर्शी हैं, वे इन मार्गों को अलग नहीं मानते। वे समझते हैं कि दोनों मार्ग भीतर की शुद्धि और परम की प्राप्ति की दिशा में जाते हैं।
प्रतीकात्मक अर्थ:
- सांख्य — बुद्धिवादी, विवेकपूर्ण आत्मनिरीक्षण का मार्ग
- योग — समर्पण और कर्म में साम्यभाव का मार्ग
- बालाः — जो केवल बाह्य आचरण को देखते हैं, जो आध्यात्मिकता की गहराई नहीं समझते
- पण्डिताः — वे जो आत्मा, ब्रह्म और जीवन के रहस्यों को जानने वाले हैं
- एकमप्यास्थितः — जो एक मार्ग को निष्ठा, श्रद्धा और विवेक से अपनाता है
- फलम् — आत्मसाक्षात्कार, मोक्ष, परमशांति
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा:
- मार्ग की तुलना नहीं, उसका अनुसरण महत्वपूर्ण है — चाहे कोई ज्ञान मार्ग चुने या कर्म मार्ग, आवश्यक है कि उसमें दृढ़ रहे और उसे समर्पणपूर्वक निभाए।
- ज्ञान और कर्म में भेद केवल दृष्टिकोण का है — कोई भी मार्ग यदि श्रद्धा और शुद्ध चित्त से अपनाया जाए, तो अंततः वही फल देता है।
- अनुभव से सत्य की प्राप्ति होती है — बालबुद्धि वाले लोग तर्क और सतही भेद पर अटक जाते हैं, परंतु पण्डित जन तटस्थ और समदर्शी होते हैं।
- समर्पण और निष्ठा की आवश्यकता — एक भी मार्ग यदि दृढ़तापूर्वक अपनाया जाए, तो वह पूर्णता तक ले जाता है।
- आंतरिक समरसता — व्यक्ति को अपने भीतर ज्ञान और कर्म के संतुलन को विकसित करना चाहिए। केवल ज्ञान या केवल कर्म से जीवन में पूर्णता नहीं आती।
आत्मचिंतन के प्रश्न:
क्या मैं ज्ञान और कर्म को अलग-अलग मानकर भ्रमित तो नहीं हूँ?
क्या मैं अपने चुने हुए मार्ग पर समर्पण और निष्ठा से चल रहा हूँ?
क्या मेरे दृष्टिकोण में गहराई है, या मैं सतही स्तर पर रहकर दूसरों के मार्गों की आलोचना करता हूँ?
क्या मुझे यह बोध हुआ है कि सब मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर जाते हैं?
क्या मेरे कर्म और विचार एक-दूसरे के पूरक हैं या उनमें विरोध है?
निष्कर्ष:
इस श्लोक का सार यही है कि सत्य तक पहुँचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी एक मार्ग को दृढ़ता से अपनाते हैं, तो वह हमें परम लक्ष्य तक पहुँचाता है। श्रीकृष्ण यहाँ भ्रम को दूर करते हैं और बताते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों एक ही लक्ष्य के साधन हैं।
जो लोग दोनों को भिन्न-भिन्न और विरोधी मानते हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि से अभी अपरिपक्व हैं। जबकि जो समझते हैं कि दोनों पथों का लक्ष्य आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मबोध है, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं।
हमें अपने मार्ग को चुनकर उस पर सत्य, श्रद्धा और साधना के साथ चलना चाहिए, बिना यह सोचे कि कोई अन्य मार्ग श्रेष्ठ या हीन है। यदि हम एक मार्ग में भी पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो हम वही फल पाते हैं — आत्मिक शांति, मुक्ति और परम सत्य का साक्षात्कार।
अंतिम भावना:
ज्ञान और कर्म, दोनों जब संतुलित रूप में जीवन में उतरते हैं, तो वे जीवन को दिव्यता की ओर ले जाते हैं। जैसे दो नदियाँ एक महासागर में मिलती हैं, वैसे ही यह दोनों मार्ग परमात्मा के सागर में ले जाकर मिला देते हैं।
