मूल श्लोक – 8
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपश्वसन् ॥8॥
शब्दार्थ:
- न एव — वास्तव में नहीं
- किञ्चित् करोमि — मैं कुछ भी करता हूँ
- इति — ऐसा
- युक्तः — योगयुक्त, समभाव में स्थित
- मन्येत — समझता है, मानता है
- तत्त्ववित् — तत्व को जानने वाला, ब्रह्मज्ञान से युक्त
- पश्यन् — देखता हुआ
- शृण्वन् — सुनता हुआ
- स्पृशन् — छूता हुआ
- जिघ्रन् — सूंघता हुआ
- अश्नन् — खाता हुआ
- गच्छन् — चलता हुआ
- स्वपन् — सोता हुआ
- श्वसन् — साँस लेता हुआ
कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते-फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए
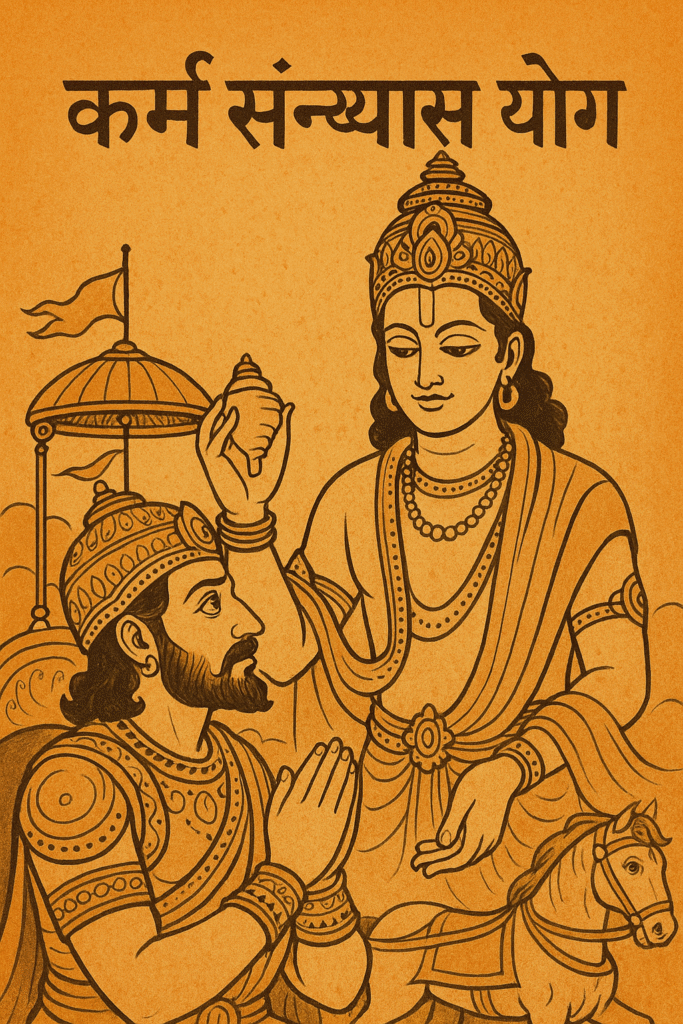
विस्तृत भावार्थ:
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कर्म और आत्मा के संबंध की गहराई को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है — जो “तत्त्ववित्” है, अर्थात आत्मा और शरीर का भेद जानता है — वह यह अनुभव करता है कि ‘मैं’ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।
हालाँकि उसकी इंद्रियाँ कार्य कर रही होती हैं — देखना, सुनना, छूना, सूँघना, खाना, चलना, सोना और श्वास लेना — पर वह समझता है कि ये सब केवल शरीर और इंद्रियों के स्तर पर हो रहा है, आत्मा तो निष्क्रिय, साक्षी है।
यह दृष्टिकोण आत्मा और शरीर के भेद का वास्तविक अनुभव है, जो केवल गूढ़ योगसाधना और ज्ञान से प्राप्त होता है। यह कर्म से विमुख नहीं है, बल्कि कर्म में अनासक्ति और साक्षीभाव को प्रकट करता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण:
- कर्तापन का अभाव — तत्वज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ‘कर्ता’ वह नहीं है, कर्ता केवल प्रकृति है (इंद्रियाँ, मन, शरीर)। आत्मा तो केवल दर्शक है।
- साक्षीभाव — “मैं देख रहा हूँ”, यह अहं का भाव है। ज्ञानी समझता है कि यह सब शरीर-मन की क्रियाएँ हैं। आत्मा केवल देख रही है, भाग नहीं ले रही।
- गुह्य योगदृष्टि — इस श्लोक में भगवान कर्मयोग की चरम अवस्था को बताते हैं — जहाँ कर्म करते हुए भी कर्तापन की भावना नहीं रहती।
- अद्वैत का प्रतिबिंब — यह भाव द्वैत को मिटाकर आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कराता है। जब अहं का विलय होता है, तब ही यह समझ आ सकती है।
प्रतीकात्मक अर्थ:
- तत्त्ववित् — वह व्यक्ति जो आत्मा को न कर्ता मानता है, न भोक्ता; केवल साक्षी।
- युक्तः — मन, बुद्धि, इंद्रियाँ और आत्मा में समन्वय प्राप्त कर चुका योगी।
- कर्म की निरपेक्षता — कर्म तो चलता रहता है, पर ज्ञानी उस कर्म से स्वयं को अलग मानता है।
- इंद्रिय क्रियाएँ — केवल शरीर का स्वाभाविक कार्य; आत्मा अप्रभावित रहती है।
- “मैं कुछ नहीं करता” — यह त्याग नहीं, बल्कि परमज्ञान की स्थिति है।
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा:
- कर्ताभाव का त्याग — जब हम समझते हैं कि ‘मैं’ नहीं बल्कि प्रकृति कर्म कर रही है, तभी सच्चा योग आरंभ होता है।
- कर्म में रहकर भी निर्लिप्तता — यही कर्मयोग का सार है — कर्म करो, पर ‘मैं’ करने वाला नहीं हूँ, यह अनुभव करो।
- साक्षीभाव का अभ्यास — अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि को एक साक्षी की तरह देखना — यह ध्यान की सबसे उन्नत अवस्था है।
- आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव — जब ‘मैं’ की सीमा टूटती है, तब ही आत्मा की असीमता का अनुभव होता है।
- आंतरिक शांति और मुक्ति — जब हम कर्ता नहीं, केवल साक्षी होते हैं, तो चिंता, भय, मोह समाप्त हो जाते हैं।
आत्मचिंतन के प्रश्न:
क्या मैं अपने कार्यों को ‘मैं कर रहा हूँ’ की भावना से करता हूँ?
क्या मुझे शरीर और आत्मा के भेद का अनुभव है या केवल ज्ञान के स्तर पर समझ है?
क्या मैं अपने दिनचर्या के हर कार्य में साक्षीभाव रख पाता हूँ?
क्या मेरी इंद्रियाँ मेरे नियंत्रण में हैं या मैं उनके पीछे चल रहा हूँ?
क्या मैंने कभी यह गहराई से सोचा है कि ‘मैं कौन हूँ?’ — शरीर, मन, या आत्मा?
निष्कर्ष:
यह श्लोक हमें बताता है कि आत्मबोध की स्थिति में व्यक्ति यद्यपि सब कुछ करता हुआ प्रतीत होता है — देखना, सुनना, बोलना, चलना — फिर भी वह अनुभव करता है कि “मैं कुछ नहीं करता।” यह स्थिति केवल गहन ध्यान, आत्मचिंतन और योगाभ्यास से आती है।
जब व्यक्ति ‘कर्तापन’ का त्याग करता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। तब कर्म से बंधन नहीं होता, बल्कि कर्म ही साधन बन जाता है आत्मा की स्वतंत्रता का।
भगवद्गीता का यह श्लोक चेतना के उच्चतम स्तर की ओर हमें प्रेरित करता है — जहाँ कर्म होता है, पर कर्ता नहीं होता; जहाँ जीवन चलता है, पर ‘मैं’ केवल साक्षी रहता है। यही आत्मज्ञान की पूर्णता है।
