मूल श्लोक – 2
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ।
न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥2॥
शब्दार्थ
यं — जिसको
संन्यासम् — संन्यास, त्याग
इति — इस प्रकार
प्राहुः — कहा गया है
योगम् — योग, समत्वबुद्धि सहित कर्म
तम् — उसी को
विद्धि — जानो, समझो
पाण्डव — हे पाण्डव (अर्जुन)
न — नहीं
हि — निश्चय ही
असंन्यस्त — जो त्याग नहीं किया गया है
सङ्कल्पः — इच्छाएँ, कामनाएँ, मानसिक योजनाएँ
योगी — योगी
भवति — होता है
कश्चन — कोई भी
जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना संन्यासी नहीं बन सकता।
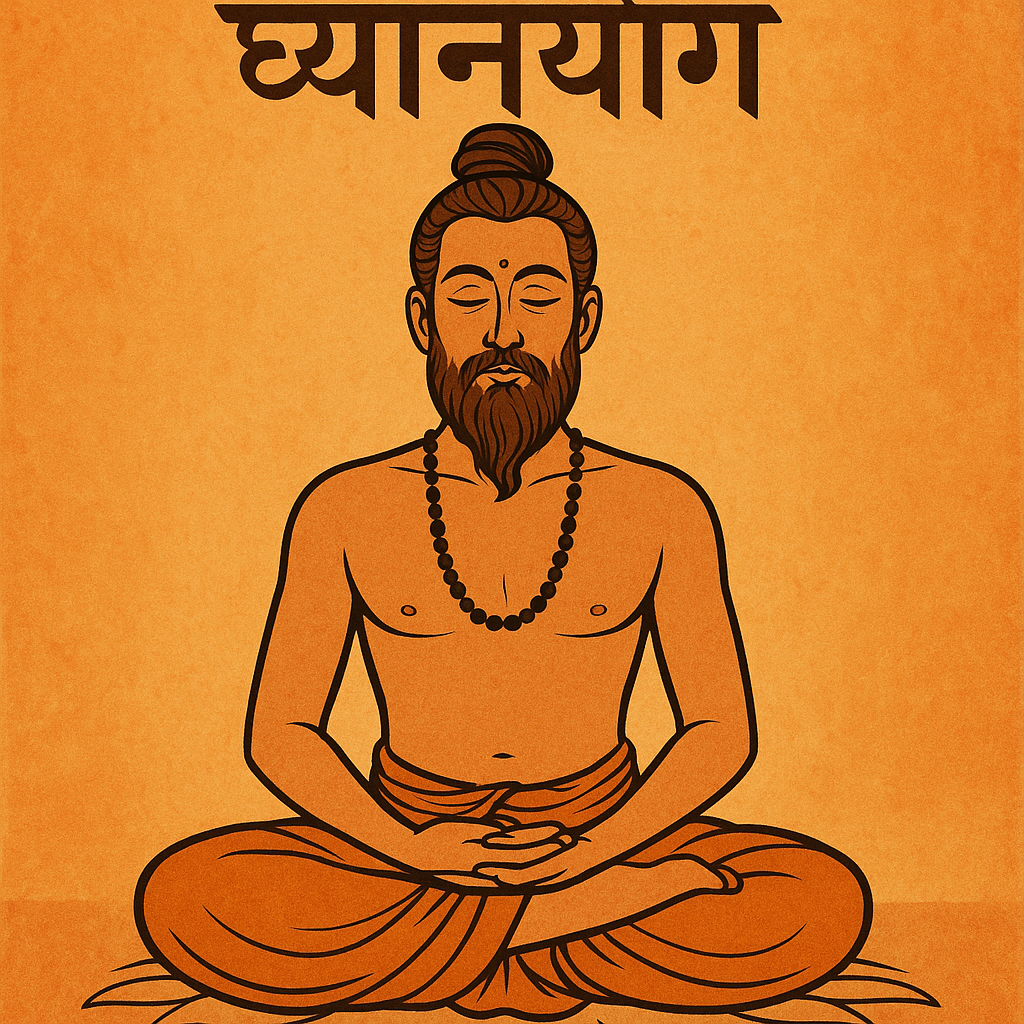
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को संन्यास और योग की एकरूपता का बोध कराते हैं। आम जन की दृष्टि में संन्यास का अर्थ है – संसार का त्याग करना, वस्त्र बदल लेना, गृह त्याग देना। किंतु भगवान गीता में संन्यास को संकल्पों के त्याग के रूप में परिभाषित करते हैं।
यहाँ ‘संकल्प’ का अर्थ है – फल की आकांक्षा, कामनाओं की योजनाएं, “मैं यह करूँगा, वह पाऊँगा” जैसी इच्छाएँ।
योगी वही है जो ऐसे संकल्पों से मुक्त हो चुका है। कर्म करता है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करता — निष्काम भाव से। अतः सच्चा योगी वही है जो संन्यासी है, अर्थात इच्छाओं और अभिलाषाओं को त्याग चुका है, चाहे वह संसार में रहकर कार्य कर रहा हो।
दार्शनिक दृष्टिकोण
यह श्लोक कर्मयोग और ज्ञानयोग के अद्भुत समन्वय को प्रकट करता है।
- गीता का संन्यास त्याग का प्रतीक है — लेकिन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक त्याग।
- यहाँ योग का अर्थ है: समत्व बुद्धि, निष्काम भाव, मन का संयम।
- जो अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी है।
- फल की इच्छा मन को बाँधती है; उसका त्याग मन को मुक्त करता है।
इसलिए, त्याग और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं — एक त्याग करता है, दूसरा जोड़ता है — दोनों अंततः आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम हैं।
प्रतीकात्मक अर्थ
| शब्द | प्रतीकात्मक अर्थ |
|---|---|
| संन्यास | कामनाओं और इच्छाओं का आंतरिक त्याग |
| योग | जीवन में समता, संतुलन और प्रभु से जुड़ाव |
| संकल्प | मन की योजनाएं, अपेक्षाएँ और इच्छाओं की श्रृंखला |
| योगी | वह जो हर परिस्थिति में समभाव रखता है, फल की चिंता नहीं करता |
| पाण्डव | अर्जुन के माध्यम से सभी साधकों के लिए संदेश |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- त्याग कोई बाहरी कर्म नहीं, बल्कि अंतर की भावना है।
- एक गृहस्थ भी योगी हो सकता है, यदि वह निष्काम भाव से कर्म करता हो।
- इच्छाओं का त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता है।
- योग कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि मन की स्थिति है — समता और संतुलन।
- जो अपने संकल्पों को त्याग नहीं पाता, वह ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता।
आत्मचिंतन के प्रश्न
- क्या मैं अपने कर्मों को फल की इच्छा से करता हूँ, या निष्काम भाव से?
- क्या मैं इच्छाओं और संकल्पों में बंधा हूँ, या आंतरिक रूप से मुक्त हूँ?
- क्या मेरा त्याग केवल बाहरी है, या भीतर से भी आया है?
- क्या मैं हर कार्य में प्रभु की भावना से योग जोड़ पा रहा हूँ?
- क्या मेरे जीवन में योग (समत्व) और संन्यास (त्याग) दोनों हैं?
निष्कर्ष
इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और हम सभी को यह गहन संदेश देते हैं कि—
सच्चा संन्यास कर्मों से भागना नहीं है, बल्कि इच्छाओं और फल की आकांक्षा का त्याग करना है।
और यही योग है — कर्म करते हुए भी भीतर से शांत, मुक्त और प्रभु से जुड़ा हुआ। जब मनुष्य फल की आकांक्षाओं को छोड़कर समर्पित भाव से कर्म करता है, तब वह योगी भी होता है और संन्यासी भी।
यही वह पथ है जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है — जहां कोई तनाव नहीं, केवल समता, संतुलन और शांति होती है।
