मूल श्लोक – 13
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः।
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥13॥
शब्दार्थ
- समम् — सीधा, संतुलित
- काय-शिरो-ग्रीवम् — शरीर, सिर और ग्रीवा (गर्दन)
- धारयन् — धारण करते हुए
- अचलम् — अडोल, स्थिर
- स्थिरः — स्थायी, दृढ़
- सम्प्रेक्ष्य — दृष्टि केंद्रित करते हुए
- नासिकाग्रं स्वं — अपनी नाक के अग्रभाग (नाक के सिरे) पर
- दिशः च अनवलोकयन् — इधर-उधर की दिशाओं में दृष्टि न डालते हुए
उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आँखों को हिलाए बिना नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए।
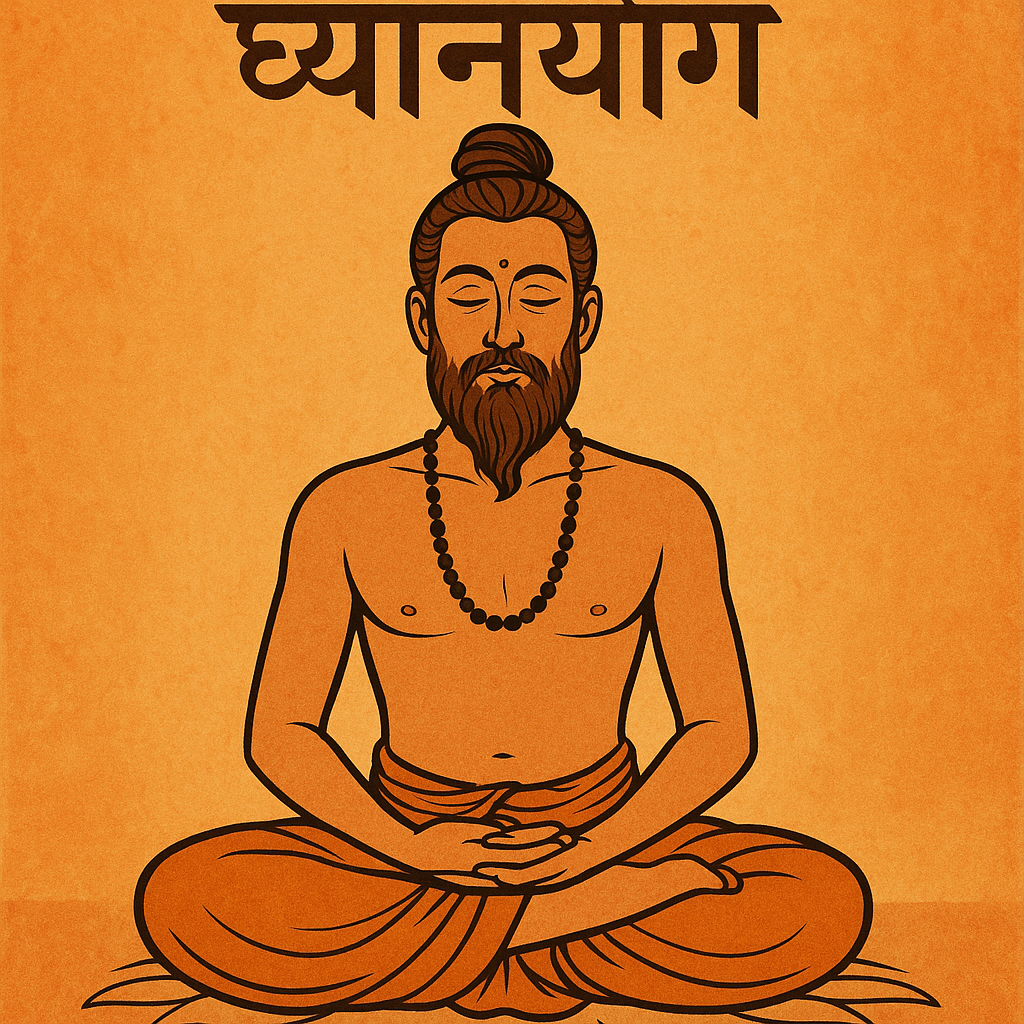
विस्तृत भावार्थ
भगवान श्रीकृष्ण ध्यान के व्यवहारिक निर्देश दे रहे हैं। योग का अभ्यास केवल मानसिक ही नहीं होता, उसमें शारीरिक स्थिति की भी अत्यंत महत्ता होती है। इस श्लोक में ध्यान की सही शारीरिक मुद्रा का वर्णन किया गया है।
ध्यान के लिए मुख्य निर्देश:
- शरीर, सिर और ग्रीवा को सीध में रखें (समं काय-शिरो-ग्रीवम्)
- यह मुद्रा शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करती है।
- इससे श्वास और प्राण की लय संतुलित होती है।
- अचलम् स्थिरः — शरीर को बिना हिलाए स्थिर रखना
- चंचलता मन में भी अशांति लाती है।
- जब शरीर स्थिर होता है, तो मन भी स्थिर होने लगता है।
- दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें (नासिकाग्रं सम्प्रेक्ष्य)
- यह एक प्रसिद्ध ध्यान विधि है — नासिकाग्रदृष्टि।
- यह ध्यान को केंद्र में लाने में सहायक है और इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाने में मदद करती है।
- दिशश्च अनवलोकयन् — इधर-उधर न देखें
- ध्यान में बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर यात्रा आरंभ होती है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- योग का उद्देश्य केवल शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि चेतना को भीतर केंद्रित करना है।
- जब शरीर, मन, और दृष्टि — तीनों स्थिर हो जाते हैं, तब आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के योग्य होती है।
- इस श्लोक में योग की एकाग्रता, स्थिरता और सजगता की महिमा बताई गई है।
- यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि ध्यान कोई भावनात्मक उड़ान नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान है।
प्रतीकात्मक अर्थ
| शब्द / अवस्था | प्रतीकात्मक अर्थ |
|---|---|
| समं काय-शिरो-ग्रीवम् | जीवन में संतुलन और स्थायित्व का भाव |
| अचलः स्थिरः | मानसिक चंचलता से परे, आत्मा की स्थिति में स्थित रहना |
| नासिकाग्रदृष्टि | इंद्रियों को नियंत्रित कर, मन को केंद्र की ओर लाना |
| दिशः अनवलोकयन् | बाहरी संसार को तिलांजलि देकर आत्मा की ओर दृष्टि केंद्रित करना |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- ध्यान के लिए सही शारीरिक स्थिति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी मानसिक एकाग्रता।
- शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता को जन्म देती है — जो अंततः आत्मा की स्थिरता तक ले जाती है।
- नासिकाग्र पर दृष्टि टिकाने से चेतना केंद्रित होती है, जिससे ध्यान गहराता है।
- बाहरी दिशाओं की ओर न देखना — यह प्रतीक है कि साधक अब बाहरी दुनिया से नाता तोड़ कर भीतर की ओर यात्रा कर रहा है।
- यह स्थिति ही योग की प्रारंभिक परिपक्व अवस्था का आरंभ है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
- क्या मैं ध्यान करते समय शरीर को स्थिर रख पाता हूँ?
- क्या मेरी दृष्टि और चेतना इधर-उधर भटकती है या केंद्रित रहती है?
- क्या मेरा मन भीतर की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है या बाहर की दिशाओं में उलझा रहता है?
- क्या मैं बाह्य चंचलता को त्याग कर आंतरिक स्थिरता को विकसित कर रहा हूँ?
- क्या मैंने ध्यान को सिर्फ मानसिक अभ्यास माना है या शारीरिक और चेतनात्मक समन्वय भी समझा है?
निष्कर्ष
यह श्लोक भगवद्गीता में ध्यानयोग की व्यवस्थित प्रक्रिया का सूक्ष्म परिचय देता है। श्रीकृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ध्यान कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण शास्त्रीय अनुशासन है, जिसमें शरीर, दृष्टि, और चेतना — तीनों को नियंत्रित कर के परमात्मा से मिलन की तैयारी होती है।
“स्थिर शरीर, स्थिर दृष्टि, और शांत चित्त — यही ध्यान का प्रवेशद्वार है।”
सार यह है:
ध्यान का प्रारंभ — शरीर से
दिशा — दृष्टि से
गहराई — चित्त से
लक्ष्य — आत्मा से परमात्मा की एकता।
यही योग है, यही जीवन की अंतर्ज्ञान यात्रा का द्वार है।
