मूल श्लोक – 10
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥10॥
शब्दार्थ:
- ब्रह्मणि — ब्रह्म (परमात्मा, सर्वोच्च चेतना) में
- आधाय — अर्पण करके, समर्पित करके
- कर्माणि — सब कर्मों को
- सङ्गं त्यक्त्वा — आसक्ति को त्यागकर
- करोति यः — जो व्यक्ति कर्म करता है
- सः — वह
- न लिप्यते — लिप्त नहीं होता, प्रभावित नहीं होता
- पापेन — पाप से, दोष से
- पद्मपत्रम् इव — कमल के पत्ते के समान
- अम्भसा — जल से
वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पापकर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता।
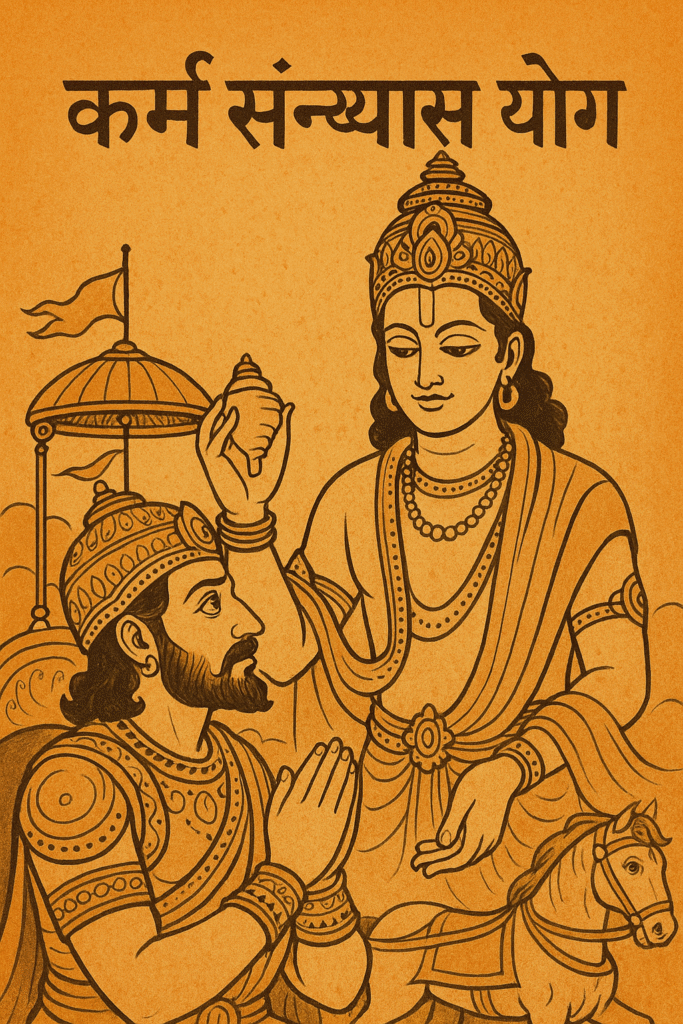
विस्तृत भावार्थ:
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कर्मयोग का सर्वोच्च सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को “ब्रह्म” अर्थात् ईश्वर को समर्पित कर देता है और उन कर्मों में आसक्ति नहीं रखता, तब वह किसी भी पाप या कर्म के बंधन से नहीं बँधता।
यह स्थिति निष्काम कर्म की होती है — जहाँ न फल की कामना है, न ही कर्म के प्रति मोह। कर्म होते हैं, पर ‘मैं’ या ‘मेरा’ का भाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का जीवन परमात्मा की सेवा बन जाता है, और वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है।
भगवान उदाहरण देते हैं — जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार ऐसा योगी कर्म करते हुए भी पाप या बंधन से अछूता रहता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण:
- कर्म का ब्रह्मार्पण — जब हम कर्म को स्वयं के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए करते हैं, तब वह कर्म शुद्ध हो जाता है।
- आसक्ति का त्याग — कर्म में उलझाव तभी होता है जब हम फल के प्रति आसक्त होते हैं। जब यह आसक्ति नहीं रहती, तो कर्म से बंधन नहीं होता।
- कर्तापन की निवृत्ति — इस स्थिति में व्यक्ति कर्ता नहीं, केवल एक निमित्त होता है। ईश्वर के आदेश से प्रेरित होकर वह कर्म करता है।
- निर्लिप्तता की अवस्था — कमलपत्ते की तरह, जो जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता।
- आत्मिक स्वतंत्रता — यह शुद्धता ही आत्मा को कर्म के संस्कारों से मुक्त करती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।
प्रतीकात्मक अर्थ:
- ब्रह्मणि आधाय — आत्मा का सबकुछ परमात्मा को समर्पित कर देना।
- सङ्गं त्यक्त्वा — कर्म करते हुए भी उससे कोई निजी स्वार्थ या लालच न रखना।
- लिप्यते न स पापेन — ऐसा व्यक्ति संसार के कर्मों में उलझकर पाप का भागी नहीं बनता।
- पद्मपत्रमिवाम्भसा — कमल के पत्ते की तरह जो जल में रहकर भी शुद्ध और अलग रहता है — यही योगी की स्थिति है।
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा:
- कर्म को ईश्वरार्पण बनाओ — यदि हम हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करें, तो वह पूजा बन जाता है।
- निष्काम भाव से कर्म करो — फल की चिंता छोड़ दो, केवल कर्म करते जाओ — यही सच्चा धर्म है।
- दुनिया में रहो, पर उसमें डूबो मत — जैसे कमल जल में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, वैसे ही योगी को रहना चाहिए।
- कर्ताभाव से मुक्त रहो — ‘मैं कर रहा हूँ’ की भावना त्यागो, ‘ईश्वर मुझसे करा रहे हैं’ यह भाव रखो।
- पवित्रता और समर्पण से जीवन जियो — तभी कर्मों का असर हमें बाँध नहीं पाएगा, और आत्मा मुक्त रहेगी।
आत्मचिंतन के प्रश्न:
क्या मैं अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करता हूँ या अहंकारवश करता हूँ?
क्या मेरे कर्म स्वार्थ से प्रेरित हैं या सेवा और समर्पण से?
क्या मैं कर्म में लिप्त हूँ या साक्षी भाव से उसे देख पाता हूँ?
क्या मैं संसार में कमल की तरह रह रहा हूँ या उसमें डूब रहा हूँ?
क्या मैं फल की चिंता करता हूँ या केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता हूँ?
निष्कर्ष:
यह श्लोक भगवद्गीता के कर्मयोग सिद्धांत का सार है। भगवान श्रीकृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कर्म करना बुरा नहीं है, पर आसक्ति और कर्ताभाव हमें बंधन में डालते हैं। जब हम कर्मों को ब्रह्म को अर्पण करके निष्काम भाव से करते हैं, तब पाप, दोष या बंधन हमसे नहीं जुड़ते।
जीवन का लक्ष्य है — कर्म करते हुए भी आत्मा को शुद्ध, निर्मल और निर्लिप्त रखना।
यह तभी संभव है जब कर्म सेवा हो, समर्पण हो, और कर्तापन से मुक्त हो।
इस प्रकार का जीवन ही वास्तविक योग है, और वही मोक्ष की ओर अग्रसर करता है।
गीता हमें कर्म का मार्ग सिखाकर मुक्ति की ओर ले जाती है — जल में रहते हुए भी कमल के पत्ते जैसा बनकर।
