मूल श्लोक – 23
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥23॥
शब्दार्थ
- शक्नोति — समर्थ होता है, सक्षम होता है
- इह एव — इसी संसार में, इसी जीवन में
- यः — जो व्यक्ति
- सोढुम् — सहन करने में, सहने में
- प्राक् — पहले, पूर्व में
- शरीरविमोक्षणात् — शरीर छोड़ने से पहले, मृत्यु से पूर्व
- काम — इच्छा, वासना
- क्रोध — गुस्सा, रोष
- उद्भवम् — उत्पन्न हुए, से जन्मा हुआ
- वेगम् — तीव्रता, वेग, आवेग
- युक्तः — संयमित, योगयुक्त
- सः सुखी नरः — वह मनुष्य सुखी है, वह आनंद को प्राप्त करता है
वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं, केवल वही संसार मे सुखी रहते हैं।
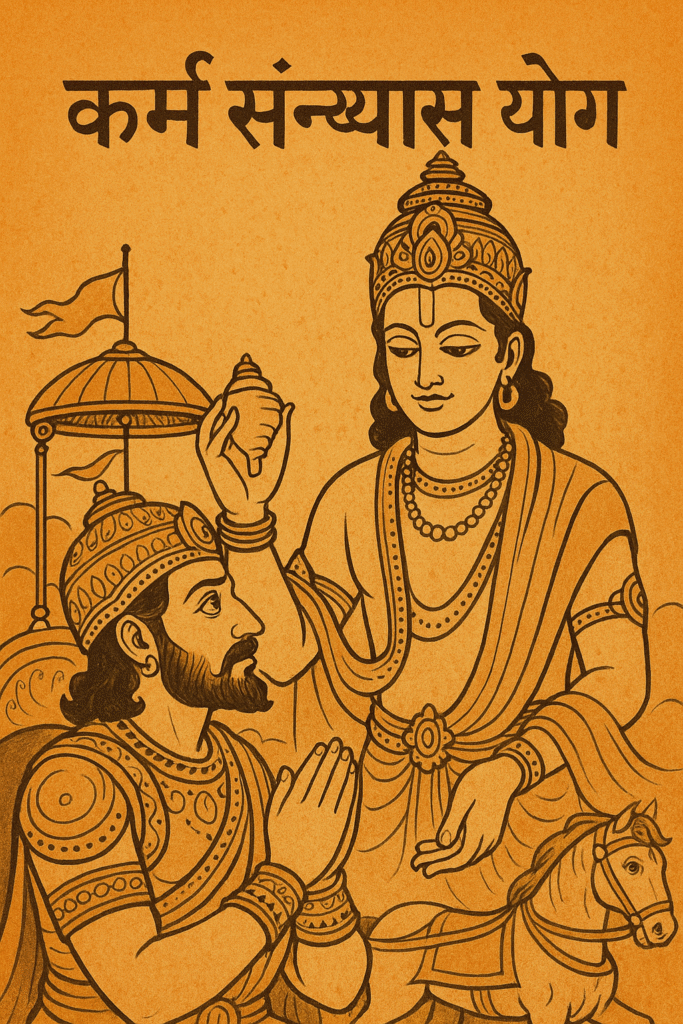
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने आत्मसंयम की महत्ता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर उत्पन्न काम (वासना) और क्रोध हैं। ये दोनों वेग (उत्तेजना) इतने तीव्र होते हैं कि साधारण मनुष्य उनका सामना नहीं कर पाता और उनके प्रभाव में आकर पाप कर्म करता है।
परंतु जो साधक योगयुक्त है, जिसका मन और इन्द्रियाँ संयमित हैं, वह इन आवेगों को पहचानकर, उन्हें रोककर आत्मनियंत्रण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए ही मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है और सच्चा सुखी बनता है।
शरीरविमोक्षणात् पूर्व — यहाँ एक अत्यंत गूढ़ बात कही गई है: यदि हम इन वेगों पर मृत्यु से पहले नियंत्रण पा लें, तो यही जीवन मुक्ति का माध्यम बन सकता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- काम और क्रोध आत्मा के विरोधी हैं:
ये दोनों मन को अंधा कर देते हैं, विवेक का नाश कर देते हैं। - सहनशीलता ही साधना है:
जो व्यक्ति इन मानसिक वेगों को सह लेता है, वह आत्मज्ञानी बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। - योग का सही अर्थ आत्मनियंत्रण है:
केवल ध्यान या पूजा नहीं, बल्कि काम-क्रोध जैसी प्रवृत्तियों पर विजय पाना ही सच्चा योग है। - इस जीवन में ही मोक्ष संभव है:
यह श्लोक स्पष्ट करता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इच्छाओं के नियंत्रण के साथ इस जीवन में संभव है।
प्रतीकात्मक अर्थ
- काम — संसार की वासनाएँ: भोग, संपत्ति, पद
- क्रोध — इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उत्पन्न होने वाला आंतरिक विष
- वेग — भावनात्मक अशांति, जो विवेक को दबा देती है
- शरीरविमोक्षण — मृत्यु का प्रतीक, या जीवन का अंतिम क्षण
- युक्त — संयमी, विवेकी, स्थिर बुद्धि वाला
- सुखी — वह जो भीतर से शांत, निर्लिप्त और आनन्दपूर्ण हो
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- सच्चा सुख संयम से आता है:
बाह्य भोग नहीं, आत्मनियंत्रण ही सुख का स्रोत है। - मन पर नियंत्रण अनिवार्य है:
यदि हम अपने भीतर के काम-क्रोध को जीत लें, तो कोई बाह्य शक्ति हमें नहीं डिगा सकती। - योग का सार आत्मसंयम है:
योग केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि मानसिक वेगों को रोकना है। - मृत्यु से पहले आत्मविजय करें:
यह जीवन ही साधना का समय है, मृत्यु के बाद कुछ भी साध्य नहीं।
आत्मचिंतन के प्रश्न
क्या मैं अपनी इच्छाओं को पहचानकर नियंत्रित कर पाता हूँ?
क्या मेरे क्रोध के कारण मैं अपने संबंधों या निर्णयों को बिगाड़ता हूँ?
क्या मैं अपने भीतर उत्पन्न आवेगों को सह सकता हूँ?
क्या मेरा मन बाहरी सुखों की ओर दौड़ता है या आत्मसुख की ओर मुड़ा है?
क्या मैं योग का अभ्यास केवल शारीरिक रूप से कर रहा हूँ, या मानसिक रूप से भी?
निष्कर्ष
यह श्लोक हमें जीवन की एक गहरी सच्चाई सिखाता है — जो भीतर उत्पन्न वेगों को सह सके, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सुखी है। काम और क्रोध वे अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें बंधन में डालती हैं। यदि हम उन्हें तोड़ सकें, तो हमारा जीवन ही मोक्ष बन सकता है।
श्रीकृष्ण की यह सीख न केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। संयम, सहनशीलता और आत्मनिरीक्षण — यही योग की सच्ची साधना है।
