मूल श्लोक – 26
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥26॥
शब्दार्थ:
- काम-क्रोध-वियुक्तानाम् — जो कामना और क्रोध से रहित हो गए हैं
- यतीनां — संयमी, तपस्वियों के
- यत-चेतसाम् — जिनका चित्त संयमित है
- अभितः — चारों ओर से, हर ओर से
- ब्रह्म-निर्वाणम् — ब्रह्म में विलीन होने की स्थिति, मोक्ष
- वर्तते — स्थित है, प्राप्त होती है
- विदित-आत्मनाम् — जिनका आत्मा का ज्ञान हुआ है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है
ऐसे संन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे भी माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।
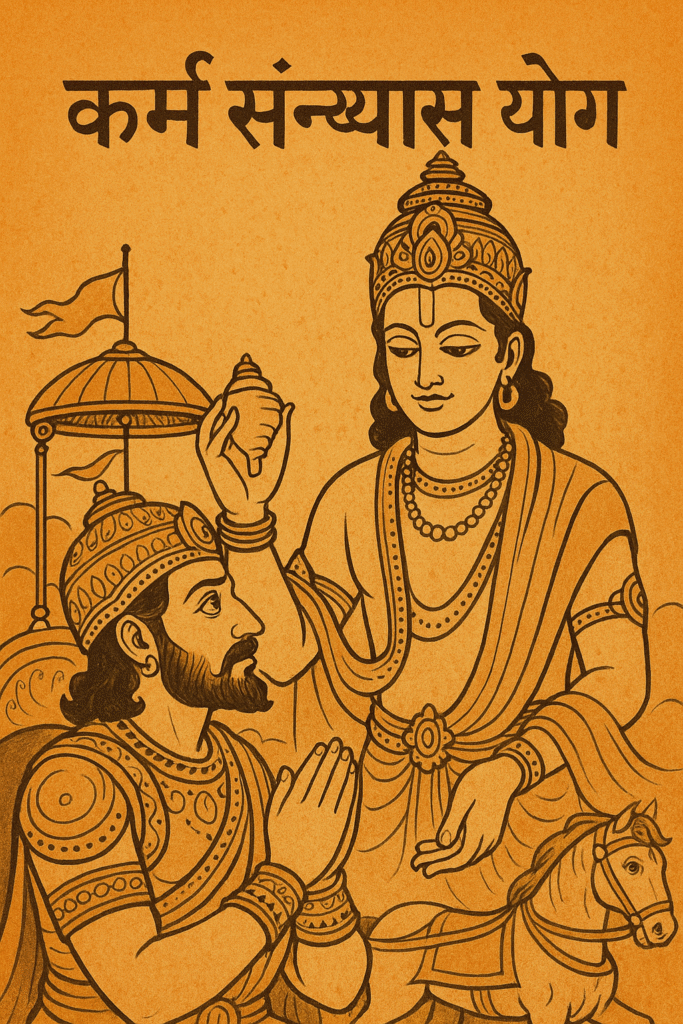
विस्तृत भावार्थ:
भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में ब्रह्म-निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करने की योग्यता को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह अवस्था उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है:
- जो काम और क्रोध से मुक्त हो चुके हैं — अर्थात् जिनकी इंद्रियाँ और मन अब वासना व गुस्से के वशीभूत नहीं होते।
- जो संयमी हैं — ऐसे साधक जिन्होंने अपने चित्त को नियंत्रित कर लिया है।
- जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है — अर्थात् वे जो आत्मा के स्वरूप को जान चुके हैं और उसमें स्थित हो गए हैं।
ऐसे साधकों के लिए ब्रह्मनिर्वाण कहीं दूर नहीं, “अभितः” — यानि चारों ओर विद्यमान है। इसका अर्थ है कि वे जब चाहें, जहाँ चाहें, उसी क्षण मोक्ष की स्थिति को अनुभव कर सकते हैं।
दार्शनिक दृष्टिकोण:
- काम और क्रोध का अंत ही मुक्ति का आरंभ है।
भगवद्गीता बार-बार बताती है कि आत्मा को जानने और उसमें स्थित होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं — कामना (desire) और क्रोध (anger)। - ब्रह्मनिर्वाण कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है।
यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्म में विलीन होना कोई मरने के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि जीवन में ही अनुभव योग्य अवस्था है। - संयम और आत्मज्ञान — मोक्ष के दो स्तम्भ हैं।
बिना संयम के और बिना आत्मा के साक्षात्कार के कोई भी व्यक्ति ब्रह्म-स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता।
प्रतीकात्मक अर्थ:
- काम — लोभ, वासना, भौतिक लालसाएँ
- क्रोध — वासनाओं में बाधा आने पर उत्पन्न होने वाला मानसिक ज्वालामुखी
- यती — जो इंद्रियों और मन को वश में कर चुका हो
- यतचित्त — स्थिर, ध्यानस्थ, शुद्ध मन
- विदितात्मा — आत्मसाक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति
- ब्रह्मनिर्वाण — आत्मा का ब्रह्म में पूर्ण एकत्व, जहाँ न द्वैत है, न भ्रम
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा:
- कामना और क्रोध मानव के बंधन के मूल कारण हैं।
जो इनसे मुक्त हो गया, वह वास्तव में आज़ाद हो गया। - ब्रह्म को जानना ही मोक्ष नहीं है — उसमें स्थित होना आवश्यक है।
सैद्धांतिक ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभूति में न बदल जाए। - संयम के बिना आत्मा की अनुभूति संभव नहीं।
इसलिए गीता बार-बार संयम, तप, साधना की महत्ता बताती है। - मोक्ष दूर नहीं है — वह हमारे चारों ओर है, बस योग्यता चाहिए उसे देखने की।
आत्मचिंतन के प्रश्न:
क्या मैं कामनाओं और क्रोध के वशीभूत होकर कार्य करता हूँ?
क्या मेरा चित्त स्थिर और संयमित है या चंचल और अशांत?
क्या मैंने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया है?
क्या मैं ब्रह्मनिर्वाण को एक भविष्य की कल्पना मानता हूँ या वर्तमान में अनुभव करने योग्य स्थिति?
क्या मैं मोक्ष की दिशा में साधना कर रहा हूँ, या केवल बाह्य धर्म में उलझा हूँ?
निष्कर्ष:
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि मोक्ष, ब्रह्म से एकता, केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो काम और क्रोध जैसे मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं।
ऐसे साधक के लिए मोक्ष कोई कल्पना नहीं, बल्कि यथार्थ होता है। वह संसार में रहते हुए भी ब्रह्म का अनुभव करता है और हर क्षण में ब्रह्म में स्थित रहता है।
वास्तविक मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है।
काम, क्रोध से मुक्त होकर, आत्मा में स्थित होकर ही ब्रह्म का अनुभव संभव है।
जो ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है।
