मूल श्लोक – 17
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥17॥
शब्दार्थ
- युक्त-आहार-विहारस्य — जिसका आहार और विहार (चलना-फिरना, रहन-सहन) संतुलित है
- युक्त-चेष्टस्य कर्मसु — जिसके सभी कर्म संयमित और मर्यादित हैं
- युक्त-स्वप्न-अवबोधस्य — जिसकी नींद और जागरण का संतुलन है
- योगः — योग (ध्यान, आत्मानुशासन)
- भवति — होता है, बनता है
- दुःख-हा — दुखों को नष्ट करने वाला
लेकिन जो आहार और आमोद-प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं।
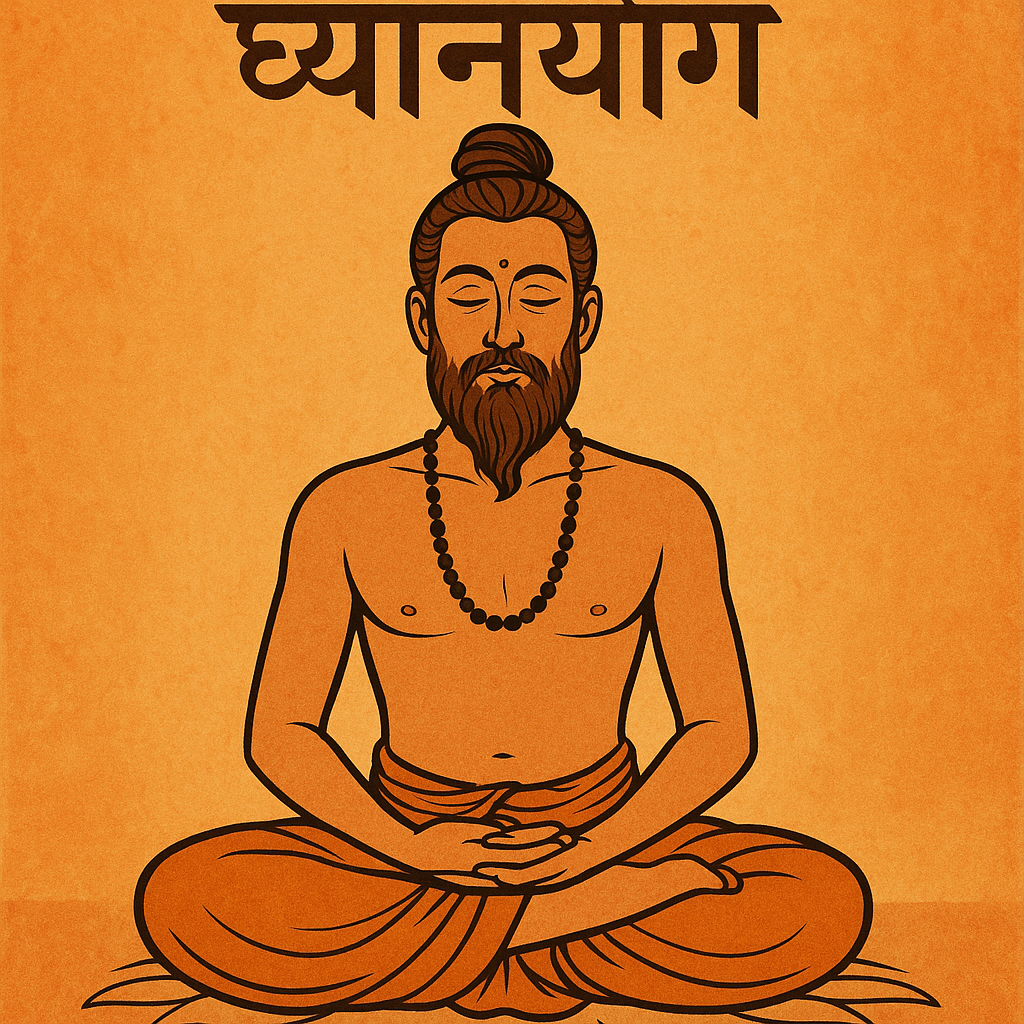
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण योग की सफलता के लिए आवश्यक जीवन-शैली का निर्देश देते हैं। ध्यान या साधना तब ही सफल होती है जब जीवन के सभी पहलुओं में मध्यमार्ग या संयम अपनाया जाए।
यहाँ पाँच “युक्तता” (संयम और संतुलन) को बताया गया है:
- युक्त आहार — न बहुत अधिक, न बहुत अल्प।
- पोषणयुक्त, सात्विक भोजन जो शरीर को सुगमता से पचे और ध्यान में बाधा न बने।
- अनियमित, भारी, या तामसिक भोजन मन को अशांत करता है।
- युक्त विहार — रहन-सहन और घूमना-फिरना भी संयमित होना चाहिए।
- न अत्यधिक शारीरिक थकान, न अत्यधिक आलस्य।
- शरीर की गति और विश्राम का संतुलन आवश्यक है।
- युक्त चेष्टा कर्मसु — कर्म और गतिविधियाँ संतुलित हों।
- कार्य में लिप्तता हो, पर आसक्ति नहीं।
- सेवा और कर्तव्य के साथ आत्मसाधना का संतुलन।
- युक्त स्वप्न — न बहुत अधिक नींद, न बहुत कम।
- अत्यधिक निद्रा मन को जड़ बना देती है।
- निद्रा का संतुलन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
- युक्त अवबोधन — जागरण का संतुलन।
- पूरी तरह सतर्क, परंतु अत्यधिक उत्तेजना से मुक्त।
- जागरण में भी सहजता और सजगता का मेल हो।
जब ये सभी पहलू संतुलित हो जाते हैं, तब योग वास्तविक दुःखहारी साधन बनता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- यह श्लोक योग को केवल आसन या ध्यान की प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि इसे संपूर्ण जीवनशैली का विज्ञान घोषित करता है।
- अति सर्वत्र वर्जयेत् — यह नीति गीता में बार-बार दोहराई जाती है।
- योग का वास्तविक उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध, और वह तभी संभव है जब शरीर और मन संतुलित और स्वस्थ हों।
- असंयमित जीवनशैली — जैसे रातभर जागना, अनियमित भोजन, आलस्य, अथवा अतिश्रम — योग साधना को असफल कर देती है।
- इसलिए संयम ही योग की भूमि है।
प्रतीकात्मक अर्थ
| शब्द / वाक्यांश | प्रतीकात्मक अर्थ |
|---|---|
| युक्त आहार | मन और शरीर को संयमित ऊर्जा देना |
| युक्त विहार | जीवन में गतिशीलता और विश्राम का संतुलन |
| युक्त चेष्टा | कर्म की गति में आत्म-स्मरण और विवेक |
| युक्त स्वप्न | आत्मा को विश्राम देने का साधन, न कि प्रमाद |
| युक्त अवबोधन | जाग्रत अवस्था में आत्म-जागरूकता |
| दुःखहा योग | ऐसा योग जो न केवल मन को शांति देता है, बल्कि जीवन की पीड़ाओं को मिटा देता है |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- सच्चा योगी वह है जो हर क्षेत्र में संयम का पालन करता है।
- केवल ध्यान लगाना पर्याप्त नहीं, जीवन की संपूर्ण गतिविधियाँ भी योग के अनुकूल होनी चाहिए।
- संयम ही आत्मबल है, और आत्मबल ही आत्मज्ञान की ओर ले जाता है।
- दुःख का कारण असंतुलन है — शरीर में, मन में, जीवन में।
- संतुलन = समत्व = योग = मुक्ति।
आत्मचिंतन के प्रश्न
- क्या मेरा भोजन योग के अनुकूल है या वासनाओं के अधीन?
- क्या मैं अति विश्राम या अति कार्य में फंसा हुआ हूँ?
- क्या मेरे कर्म संयमित और विवेकशील हैं या स्वार्थपूर्ण और आवेशित?
- क्या मेरी नींद आवश्यक और शुद्ध है या प्रमादजनित?
- क्या मैं जाग्रत अवस्था में भी आत्म-चेतना बनाए रखता हूँ?
निष्कर्ष
भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि योग कोई एक विशेष अभ्यास नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन की समग्र पद्धति है।
“जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन हो, तो ध्यान में गहराई आती है।
और जब ध्यान गहरा होता है, तो दुःख स्वयं विलीन हो जाते हैं।”
सार तत्व यह है:
योग = संयम + सजगता + समत्व
और यह योग ही है जो मनुष्य को दुःखों से मुक्त करता है, परम शांति और संतोष का द्वार खोलता है।
