मूल श्लोक – 21
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥21॥
शब्दार्थ
- सुखम् — आनंद, परम शांति
- आत्यन्तिकम् — अंतिम, अनन्त, परम
- यत् तत् — वह जो
- बुद्धिग्राह्यम् — बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जा सकता है
- अतीन्द्रियम् — इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता
- वेत्ति — जानता है, अनुभव करता है
- यत्र — जिस स्थिति में
- न च एव अयम् — यह (मनुष्य) कभी भी नहीं
- स्थितः — स्थित होकर
- चलति — विचलित होता है
- तत्त्वतः — वास्तविकता से, तत्व रूप से
योग में चरम आनन्द की अवस्था को समाधि कहते हैं जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनन्द प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपथ नहीं होता।
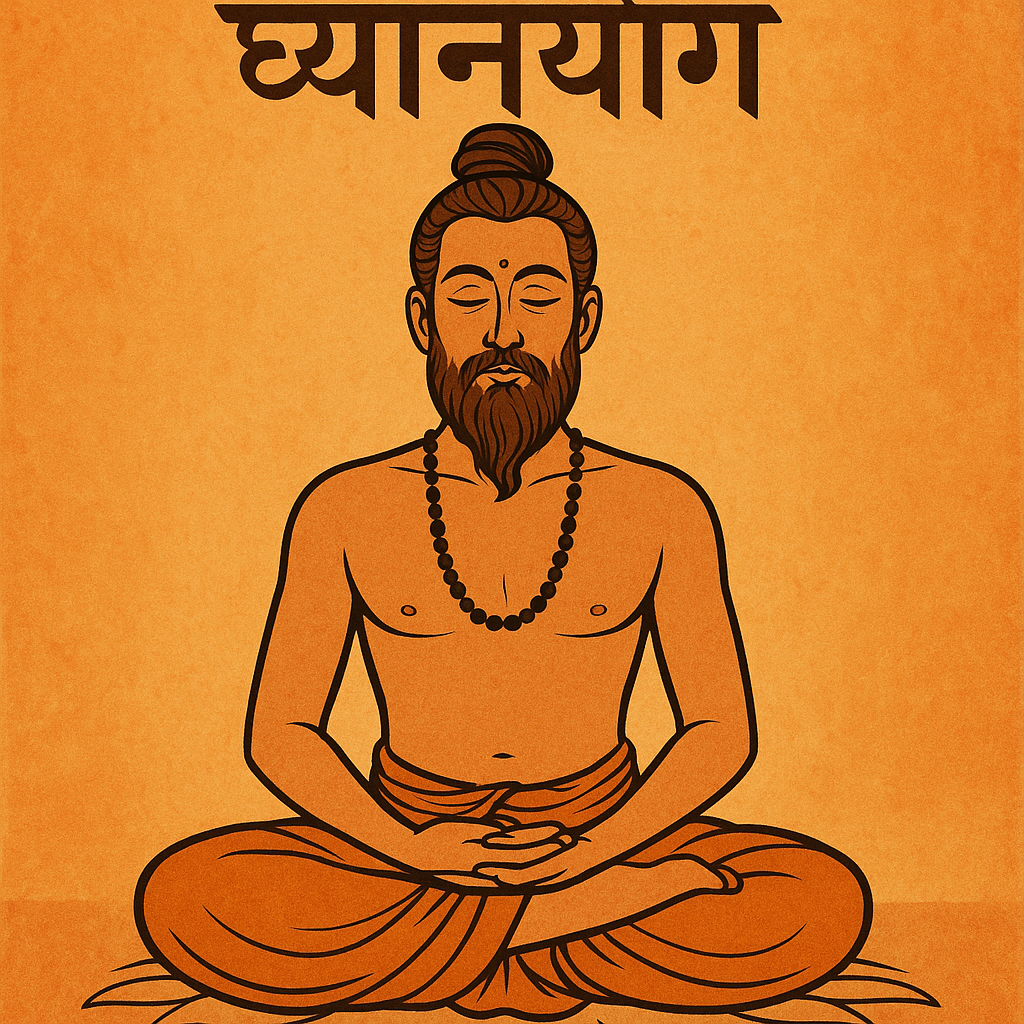
विस्तृत भावार्थ
इस श्लोक में श्रीकृष्ण ध्यानयोग की चरम स्थिति — समाधि या आत्मानुभूति — का सटीक वर्णन करते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ साधक इंद्रियातीत आनंद (Transcendental Bliss) को अनुभव करता है।
आइए इस अनुभव को चरणबद्ध समझें:
- सुखम् आत्यन्तिकम् —
- यह सुख कोई क्षणिक या भौतिक सुख नहीं है।
- यह नाशरहित, शाश्वत, अनंत और सर्वोच्च आनंद है।
- इसे आत्मसुख या ब्रह्मानंद कहा जा सकता है।
- बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् —
- यह सुख इंद्रियों द्वारा नहीं, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अनुभव किया जाता है।
- यह कोई दृश्य, स्वाद, गंध या ध्वनि नहीं है, बल्कि आत्मिक अनुभूति है।
- वेत्ति —
- योगी इस अवस्था को स्वानुभव से जानता है, यह केवल शास्त्रों में पढ़ने की चीज़ नहीं है।
- यह ज्ञान से अधिक साक्षात्कार है।
- स्थितः न चलति तत्त्वतः —
- इस स्थिति में स्थित योगी तत्वबोध से कभी विचलित नहीं होता।
- वह जान चुका होता है कि “मैं आत्मा हूँ” और फिर वह इस सत्य से हटता नहीं है।
यह वही अनुभव है जिसे सिद्ध अवस्था, समाधि, या ब्रह्म स्थिति कहा जाता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण
- गीता यहाँ पर यह स्पष्ट करती है कि मोक्ष या आत्मबोध कोई कल्पना या भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभूति है।
- यह अनुभव इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से परे ध्यान द्वारा प्राप्त होता है।
- जब साधक इस स्थिति में आता है, तो वह शाश्वत सत्य से जुड़ जाता है और फिर वह कभी संसार के द्वंद्वों से विचलित नहीं होता।
- यह अवस्था निर्विकल्प समाधि की भी संज्ञा पा सकती है — जहाँ केवल “स्व” रह जाता है, “अन्य” कुछ नहीं।
प्रतीकात्मक अर्थ
| शब्द / वाक्यांश | प्रतीकात्मक अर्थ |
|---|---|
| आत्यन्तिक सुख | ऐसा सुख जो कभी नष्ट नहीं होता — ब्रह्मानंद, आत्मानंद |
| अतीन्द्रिय | जो भौतिक इंद्रियों से परे है — सूक्ष्म, आध्यात्मिक अनुभव |
| बुद्धिग्राह्य | जो केवल सूक्ष्म अंतर्बुद्धि से समझा और अनुभव किया जा सकता है |
| स्थितः न चलति | ऐसा साधक जो आत्मज्ञान में स्थित होकर डिगता नहीं |
| तत्त्वतः | तत्वज्ञान की दृष्टि से — आत्मा के शुद्ध बोध में |
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा
- भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, आत्मिक सुख शाश्वत होता है।
- जो योगी इंद्रियों से परे जाकर आत्मा का अनुभव करता है, वही वास्तव में मुक्त होता है।
- बुद्धि जब चित्त के साथ योग में स्थित होती है, तब वह ब्रह्मसाक्षात्कार कर सकती है।
- एक बार आत्मा में स्थित हो जाने के बाद साधक कभी भी भीतर से डिगता नहीं है।
- यही स्थिरता जीवन में अडोल शांति और आनंद का मूल कारण बनती है।
आत्मचिंतन के प्रश्न
- क्या मैंने कभी ऐसा आनंद अनुभव किया है जो इंद्रियों से परे हो?
- क्या मेरा ध्यान केवल मानसिक संतुलन है, या आत्मसाक्षात्कार की ओर अग्रसर है?
- क्या मेरी बुद्धि आत्मा की दिशा में केंद्रित है या विषयों की ओर?
- क्या मैं किसी स्थायी सत्य में स्थित हूँ, या परिस्थितियों के अनुसार डोलता रहता हूँ?
- क्या मैं आत्मज्ञान के अनुभव से अपरिवर्तनीय शांत स्थिति तक पहुँचा हूँ?
निष्कर्ष
यह श्लोक गीता के ध्यानयोग अध्याय का प्रकाश-स्तंभ है।
यह हमें बताता है कि —
“जब साधक इंद्रियों से परे चला जाता है, और बुद्धि आत्मा से जुड़ जाती है,
तब वह ऐसा सुख अनुभव करता है जो स्थायी है, गहन है, और जो उसे सत्य में अडोल स्थित कर देता है।”
यह अनुभव ही मोक्ष है।
यहाँ न कोई आग्रह है, न भय, न भ्रम।
केवल आत्मा और उसकी शुद्ध अनुभूति है।
यही है —
सर्वशक्तिमान के सान्निध्य का अनुभव।
शुद्ध चित्त की पूर्णता।
योग का परम लक्ष्य।
